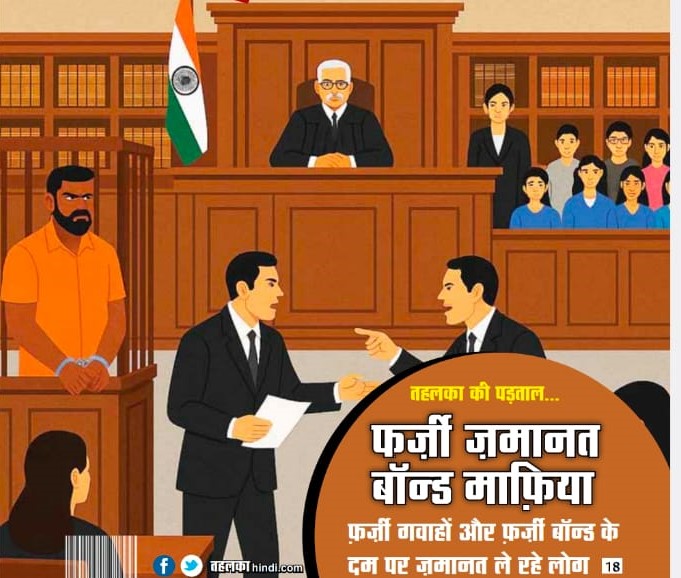भारत में न्याय में अक्सर ज़्यादा समय लगना और सुनवाई में देरी होना आम बात होने के चलते ज़मानत क़ानूनों में सुधार की माँग ज़ोर पकड़ रही है। देश की जेलों में बंद दो-तिहाई से ज़्यादा क़ैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई को तो सलाख़ों के पीछे रखा भी नहीं जाना चाहिए। उनकी निरंतर हिरासत का कारण आमतौर पर उनके कथित अपराधों की गंभीरता नहीं, बल्कि पुरानी क़ानूनी प्रणाली और सामाजिक असमानताएँ हैं। इस समस्या में एक प्रमुख रास्ता ज़मानत प्रणाली है। लेकिन इस व्यवस्था का कुछ मामलों में बेईमान तत्त्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक ज़मानत अधिनियम पारित करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसा अधिनियम, जो स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित करे, असंगतता को दूर करे और जेल नहीं, ज़मानत के संवैधानिक वादे को बेहतर ढंग से क़ायम रख सके।
‘तहलका’ के विशेष जाँच दल ने इस बार अपनी पड़ताल के दौरान ज़मानत को लेकर चौंकाने वाले तथ्य उजागर किये, जिससे पता चला कि देश में ज़मानत एक व्यवसाय बन गया है। हमारी आवरण कथा- ‘फ़र्ज़ी ज़मानत बॉन्ड माफ़िया’ में हम प्रणाली की भ्रष्ट कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाल रहे हैं, जहाँ फ़र्ज़ी गारंटर, बिचौलिये और संदिग्ध क़ानूनी पेशेवर लाभ के लिए ज़मानत प्रक्रिया में हेरफेर करते हैं। प्रभारित दरें स्थान और मामले के प्रकार जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। इससे वास्तविक और धोखाधड़ी वाली प्रथाओं के बीच का अंतर धुँधला हो जाता है, जिसमें बिचौलिये अपने लाभ के लिए दोनों पक्षों का शोषण करते हैं। न केवल वित्तीय लाभ के लिए फ़र्ज़ी ज़मानतें करायी जा रही हैं, बल्कि मानक ज़मानत प्रणाली का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है। रेलवे में बड़े पैमाने पर हुए ज़मानत बांड घोटाले की सीबीआई द्वारा हाल ही में की गयी जाँच से इस अवैध बाज़ार की जड़ें जमा लेने की प्रकृति और अधिक स्पष्ट हो गयी है।
मूलत: ज़मानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त व्यक्ति मुक़दमे के लिए वापस आये, न कि उसका अपराध सिद्ध होने से पहले उसे दंडित किया जाना। ज़मानत देने से इनकार करना एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए, जो केवल उन मामलों के लिए आरक्षित होना चाहिए, जहाँ अभियुक्त के भागने का ख़तरा हो या साक्ष्यों के साथ हस्तक्षेप कर सकता हो या गवाहों के लिए ख़तरा पैदा कर सकता हो। जब कोई मामला मुख्यत: दस्तावेज़ी साक्ष्य पर आधारित हो, तो प्रक्रियागत देरी के कारण अभियुक्त को हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। हालाँकि ज़मानत सम्बन्धी निर्णयों में विसंगतियाँ एक सतत् समस्या बनी हुई है। किसी को ज़मानत दी जाए या नहीं, और कब दी जाए; यह अक्सर मामले के गुण-दोष पर कम, जबकि न्यायिक विवेक या अभियोजन पक्ष के विरोध पर अधिक निर्भर करता है। मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमांड को मंज़ूरी देने की प्रवृत्ति के कारण स्थिति और भी ख़राब हो जाती है; विशेषकर तब, जब पुलिस द्वारा स्वत: ही अनुरोध किया जाता है।
यह जानना उत्साहवर्धक है कि पिछले सप्ताह ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर स्मारक विधि व्याख्यान के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला था कि ‘ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है।’ लेकिन इसके मूलभूत सिद्धांत को हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज़ किया गया है। यदि इसका पालन किया जाता, तो भारत की जेलों में 3.75 लाख विचाराधीन क़ैदी नहीं होते, जो कुल क़ैदियों का 74.2 प्रतिशत हैं। न्यायाधीश गवई ने अधिक सहानुभूति की आवश्यकता पर बल दिया; क्योंकि विचाराधीन क़ैदियों में से अधिकांश हाशिये के समुदायों से आते हैं। इस बीच 12 जून की दुर्घटना के बारे में भारत के विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) की रिपोर्ट ने महत्त्वपूर्ण इंजन ईंधन कट-ऑफ स्विच की स्थिति पर नये सवाल उठाये हैं। कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क़दम रखने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वापस लौट आये हैं। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। एक्सिओम-4 की यात्रा अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा द्वारा सन् 1984 में रूसी सोयुज टी-11 से उड़ान भरने के 41 वर्ष बाद हुई है।