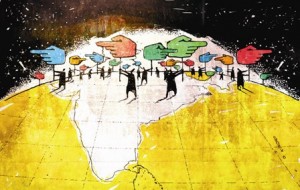 भारत आजादी के बाद के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है. या सबसे कड़े इम्तेहान से. यह कोई नाटकीय वक्तव्य नहीं है. भारत की जो कल्पना आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी के नेतृत्व में प्रस्तावित की गई थी और जिसे भारतीय संविधान ने मूर्त करने का प्रयास किया, वह पिछले एक साल में क्षत-विक्षत कर दी गई है. यह बात अब उन लोगों की समझ में भी आने लगी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत का शासन चलाने के लिए सबसे उपयुक्त पाया था और जो हाल-फिलहाल तक उसकी और उसके प्रमुख की वकालत किए जा रहे थे. अब समझ में आने लगा है कि भारत का शासन उनके हाथ में चला गया है जो पिछले सात दशकों से भारत की इस धारणा के खिलाफ जनता को तैयार कर रहे थे. फिर भी आश्चर्य की बात है कि नयनतारा सहगल को छोड़कर कोई खुलकर कहने की जरूरत महसूस नहीं करता कि भारत का शासन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है. या इतना ही कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के पास है. और यह तब भी नहीं कहा जा रहा है जब पूरा देश देख चुका है कि पूरी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में हाजिर हुई, उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और उससे निर्देश लिए. इसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष और उदार तवलीन सिंह, सुरजीत भल्ला या मेघनाद देसाई लगातार प्रधानमंत्री को सलाह दिए जा रहे हैं कि वे अपनी छवि बचा लें, जो कुछ भी हो रहा है, उससे खुद को अलग करके. या तो वे राजनीतिक मूढ़ हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं.
भारत आजादी के बाद के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है. या सबसे कड़े इम्तेहान से. यह कोई नाटकीय वक्तव्य नहीं है. भारत की जो कल्पना आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी के नेतृत्व में प्रस्तावित की गई थी और जिसे भारतीय संविधान ने मूर्त करने का प्रयास किया, वह पिछले एक साल में क्षत-विक्षत कर दी गई है. यह बात अब उन लोगों की समझ में भी आने लगी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत का शासन चलाने के लिए सबसे उपयुक्त पाया था और जो हाल-फिलहाल तक उसकी और उसके प्रमुख की वकालत किए जा रहे थे. अब समझ में आने लगा है कि भारत का शासन उनके हाथ में चला गया है जो पिछले सात दशकों से भारत की इस धारणा के खिलाफ जनता को तैयार कर रहे थे. फिर भी आश्चर्य की बात है कि नयनतारा सहगल को छोड़कर कोई खुलकर कहने की जरूरत महसूस नहीं करता कि भारत का शासन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है. या इतना ही कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के पास है. और यह तब भी नहीं कहा जा रहा है जब पूरा देश देख चुका है कि पूरी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में हाजिर हुई, उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और उससे निर्देश लिए. इसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष और उदार तवलीन सिंह, सुरजीत भल्ला या मेघनाद देसाई लगातार प्रधानमंत्री को सलाह दिए जा रहे हैं कि वे अपनी छवि बचा लें, जो कुछ भी हो रहा है, उससे खुद को अलग करके. या तो वे राजनीतिक मूढ़ हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं.
आजादी के बाद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेज शासित भूभाग से इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बनने के बावजूद हिंदुओं को इस बात के लिए सहमत करना कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आधुनिक समय में समाज के संगठन का सबसे सभ्य और मानवीय तरीका है! और अल्पसंख्यक मुसलमानों को भरोसा दिलाना कि उनके साथ धोखा नहीं होगा, वे बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ बराबरी और इज्जत के साथ रह सकेंगे. यह बीसवीं सदी के एक बड़े खून-खराबे के बीच मुमकिन हुआ. याद रखें, हिंदुओं को कोई इस्लामी राष्ट्र की सेना नहीं मार रही थी और न मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र की सेना मार रही थी, साधारण हिंदू और मुस्लिम जनता ने ही एक-दूसरे का कत्ल किया था.
गुस्से, नफरत और बदले की इस आग के बीच धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत के प्रस्ताव को व्यापक जन सहमति दिलाना आसान न था. न सिर्फ गांधी, नेहरू, आजाद जैसे नेता इसे लेकर ईमानदारी से प्रतिबद्ध थे बल्कि वे इसके लिए सामान्य जन से कड़ी बहस करने को और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे. पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने अपनी हिचक पर काबू पा लिया था और बुनियादी मानवीयता में उनकी आस्था पर संदेह नहीं किया जा सकता था.
गांधी ने अपना जनतांत्रिक प्रशिक्षण किया था, इसलिए कट्टर शाकाहारी होते हुए भी उन्हें न सिर्फ मांसाहारियों, बल्कि गोमांसाहारियों से भी कभी नफरत नहीं हुई
धर्मनिरपेक्षता को सहकारी जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत जीवन मूल्य मानने के लिए ये नेता कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे. ध्यान रहे, इनमें से अगर कोई भी खुद को हिंदू नेता के रूप में पेश करता तो भारत के सभी हिंदू उसे हाथो-हाथ लेने को तैयार थे. इस प्रलोभन को उन्होंने ठुकराया. इसमें सब शामिल थे, बावजूद पटेल और राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रमुख भूमिका निभाने के, उनके बारे में भी यह कहा जा सकता है. गांधी से सावरकर या हेडगेवार प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे और न नेहरू से. पटेल, राजेंद्र प्रसाद या अन्य नेताओं की बात ही जाने दें.
आखिर मुस्लिम लीग यही तो कह रही थी कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है. पाकिस्तान के निर्माण के बाद इसे आरोप की जगह नियति के रूप में स्वीकार करना कांग्रेस के लिए सबसे सुविधाजनक होता. शायद तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी इसे ही अवश्यसंभावी मान लेता. आखिर एक पिछड़े समाज से और क्या उम्मीद की जा सकती थी? गांधी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस ने यह आसान रास्ता नहीं चुना तो इसका अर्थ क्या था और है? इस पर हमने कायदे से विचार क्यों नहीं किया है?
धार्मिक राष्ट्र एक आसान और समझ में आने वाली कल्पना थी. आधुनिक जनतंत्रों ने भी खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित नहीं किया था. भारत के नेता बहुत मुश्किल घड़ी में यह प्रस्ताव भारत की जनता के सामने रख रहे थे.
स्वाभाविक यह था कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाने दिया जाता. गांधी और नेहरू को यह कबूल न था. गांधी ने तो तैयारी कर रखी थी कि वे नई खींची सीमा के इस ओर भगाए गए हिंदुओं और सिखों को वापस उस तरफ ले जाने और इस तरफ से खदेड़े या भागे मुसलामानों को इधर वापस लाने का अभियान चलाएंगे. आबादियों को उनके अपने परिवेश से जबरन उखाड़ दिए जाने का विचार उनके लिए असभ्यता था.
इस प्रतिबद्धता के लिए गांधी को सजा दी गई. लेकिन उनकी हत्या ने भारत की जनता को झटका दिया. यह कहा जा सकता है कि गांधी के खून ने भारत को जोड़ने का काम किया. राष्ट्रपिता की हत्या के अपराधबोध के कारण भारत में एक आत्म-चिंतन और मंथन शुरू हुआ.
भारत के इस विचार में दूसरी कई अपूर्णताएं थीं. मसलन, जैसा शिव विश्वनाथन ने अपने दिलचस्प काल्पनिक संवाद में दिखाया है यह आदिवासियों के नजरिये को समझ नहीं पाया था. लेकिन इस तरह की कमियों के बावजूद एक बड़ा हासिल इसका यह था कि इसने दो बड़ी आबादियों, यानी हिंदू और मुसलमानों को एक-दूसरे के पड़ोस में रहने को तैयार कर लिया था.
धर्मनिरपेक्षता एक अत्यंत परिष्कृत विचार था. क्या मुख्यतया निरक्षर जनता इसका अभ्यास कर पाएगी? क्या वह एक झटके में मिले सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का भी विचारपूर्वक प्रयोग कर पाएगी? इसे लेकर पश्चिम में गहरा शक था और आशंका जताई जा रही थी कि शुरुआती उत्साह के ठंडा पड़ते ही भारत बिखर जाएगा, लेकिन भारत जम गया, सार्वजनीन वयस्क मताधिकार का प्रयोग भी शिक्षा, संपन्नता, जाति-धर्म, लिंग से निरपेक्ष भारत की जनता ने प्रायः सफलतापूर्वक किया. उसका दायरा बढ़ता ही गया और उसमें नई जनता शामिल होकर उसपर अपना दावा पेश करती रही. इस अधिकार के अपहरण का इतिहास है लेकिन धीरे-धीरे दलित, आदिवासी, औरतों, सबने इसका अपने फैसले के मुताबिक इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाई. वर्चस्वशाली वर्गों से उन्हें टकराना पड़ा लेकिन उनके साथ संविधान खड़ा था. यह कितना क्रांतिकारी विचार था और कितना साहसी, यह सिर्फ दुनिया के सभी जनतंत्रों के इतिहास पर नजर डालकर समझा जा सकता है, जहां सभी तरह की आबादियों को बिना भेदभाव के एक साथ मताधिकार नहीं मिला और इसके लिए क्रमवार संघर्ष करना पड़ा.
भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के मूल में ठीक यही बात थी. जैसा जवाहरलाल नेहरू ने उसे परिभाषित किया, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में सामाजिक न्याय आधारभूत था. कहा जा सकता है कि यह धर्मनिरपेक्षता दरअसल राजनीतिक और सामाजिक शक्ति-संतुलन को पूरी तरह समानता के सिद्धांत के सहारे बदल देना चाहती थी.
गांधी और नेहरू को इसमें कोई दुविधा न थी कि धर्मनिरपेक्षता का आशय है बहुसंख्यकवाद का विरोध, उसके दबदबे से इनकार. यह बात गांधी ने 1947 के हिंसा भरे दौर में भी बेझिझक कही थी कि भारत में मुसलमान हिंदुओं के अनुचर होकर नहीं रहेंगे. यही बात बाद में नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र में स्पष्ट की. दोनों के सामने यह भी साफ था कि मुसलमानों का चतुराई से हिंदूकरण करने के किसी भी तिकड़म को कबूल नहीं किया जा सकता. यानी भारत को प्रतीकात्मक तरीके से भी हिंदू दिखना नहीं चाहिए.
यह सबकुछ समझना आसान न था, इस पर अमल करने की बात तो और मुश्किल थी. चूंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता आधुनिकीकरण या मानव स्वभाव के जनतंत्रीकरण से अभिन्न थी, इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मसंघर्ष की आवश्यकता थी. गांधी ने अपना जनतांत्रिक प्रशिक्षण किया था, इसलिए कट्टर शाकाहारी होते हुए भी उन्हें न सिर्फ मांसाहारियों, बल्कि गोमांसाहारियों से भी कभी नफरत नहीं हुई. वे खुद शराब नहीं पीते थे लेकिन अपने सहयोगियों को अपनी असाधारण स्थिति का लाभ उठाकर शराब पीने से उन्होंने रोका हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है.
आश्चर्य नहीं कि सनातनी, शाकाहारी गांधी के सामने जब राजेंद्र प्रसाद ने हजारों-हजार हिंदुओं के गोहत्या विरोधी अनुरोध का जिक्र किया तो गांधी को वह विचारणीय भी नहीं लगा. उन्होंने पूछा कि क्या हम कबूल करेंगे कि पाकिस्तान हिंदुओं पर शरीयत लागू कर दे.
धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप की जटिलता को नजरअंदाज करके इसे राजनीति से धर्म के विच्छेद की एक आधुनिकतावादी पाश्चात्य अवधारणा के रूप में समझा और प्रचारित किया गया. गांधी द्वारा धर्म के दिए व्यापक आशय को भी भुला दिया गया जिसकी आत्मा को एक संदेहवादी नेहरू ने कहीं बेहतर समझा था. धर्मनिरपेक्षता सामाजिक जीवन में साथ मिलकर रहने का नया मुहावरा गढ़ने का एक प्रयास था. इसका अभ्यास किया जाना था. सभ्य जीवन भी, जिसमें हम किसी को अपनी शक्ल में ढालने के लोभ से बचते हैं, यह दीर्घ अभ्यास का मामला था.
धर्मनिरपेक्षता में शिक्षित और संपन्न हिंदू को बहुत रुचि नहीं रही. उसने साझा सार्वजनिक स्थानों के लोप पर अफसोस नहीं किया, इसमें सक्रिय भूमिका निभाई. इस पर बहुत बात नहीं की गई है कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी के विचार के अवमूल्यन के समानांतर धर्मनिरपेक्षता का पतन भी हुआ. धर्मनिरपेक्षता का विरोध स्वार्थपरता, लालच से उपजी क्रूरता से जुड़ा हुआ है. ताज्जुब नहीं कि गुजरात के हिंदू वहां के मुसलमानों को बात करने लायक विषय भी नहीं मानते.
इसे न भूलें कि इस अभियान के साथ सार्वजनीन मताधिकार को सीमित करने के प्रयोग गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में किए जा रहे हैं. यानी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की बुनियाद, समानता को खंडित करने का प्रयास. श्रेष्ठतर भारतीय और हीनतर भारतीय की दो श्रेणियों का निर्माण.
धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का सही अनुवाद है या नहीं, इस बहस में न पड़कर यह समझने की आवश्यकता है कि यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बुनियादी सिद्धांत से संगत है, यानी सामाजिक समूहों के बीच श्रेष्ठता और हीनता के रिश्ते के अस्वीकार पर.
गांधी बावजूद औद्योगिक, वैज्ञानिक तरक्की के अंग्रेजों या यूरोपियनों को यह अधिकार देने को तैयार न थे कि वे पिछड़े हुए समाजों को सभ्य बनाएं. फिर यह अधिकार वे हिंदुओं को मुसलमानों के मुकाबले कैसे दे सकते थे? उसी तरह इस्लाम से प्रभावित होने के बावजूद अन्य धार्मिक या विश्वास-प्रणालियों से बेहतर होने के उसके दावे को वे कबूल नहीं कर सकते थे.
दादरी में हुई हत्या के प्रसंग में भारतीय राज्य की प्रतिक्रिया ने लोगों को हिला दिया है. लेकिन अब विकासवादियों को भी समझ में आ रहा है कि विकास की स्वार्थी जल्दबाजी में उन्होंने देश और खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले कर दिया है. यह समझौता उन्हें आखिरकार महंगा पड़ेगा और किस कदर, इसका पूरा अंदाजा होने में उन्हें वक्त लगे शायद. लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी?
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)





