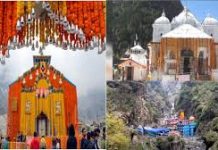काली छाया लगातार अपना विस्तार बढ़ाती जा रही है और लालकृष्ण आडवाणी के राजनीतिक जीवन का सूरज अस्ताचल के पार लपकता देखा जा सकता है. ऐसे में बाहरी दुनिया से कटे कुछ-कुछ एकांतवासियों जैसा व्यवहार कर रहे 81 वर्षीय आडवाणी निश्चित तौर पर पिछले साल छपी अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन के उन पन्नों को उलट-पुलट रहे होंगे.
मुहम्मद अली जिन्ना पर मेरी टिप्पणी पर पार्टी में जो उथल-पुथल मची उसका जिक्र मैंने अपनी जिंदगी के सबसे दुखद समय के रूप में किया है. मेरे खुद के सहयोगियों ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया
जिनको उन्होंने चुनावों में हार [2004], पार्टी में उथल-पुथल नाम दिया था. आत्मकथा का ये अध्याय काफी बेबाकी से लिखा गया है और इसमें चुनावों के बाद भारतीय राजनीति के इस महायोद्धा की मानसिक स्थिति का विस्तार से वर्णन है. वे लिखते हैं: ‘हम 2004 का संसदीय चुनाव क्यों हारे?..ये सवाल मुझे और मेरे साथियों को काफी समय तक मथता रहा. हार का कड़वा स्वाद मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है. बल्कि मेरे जीवन के शुरुआती दशकों में हार एक नियम और जीत एक अपवाद जैसी हुआ करती थी. इसने और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य और खुद पर नियंत्रण न खोने के मेरे स्वाभाविक गुण ने मेरे भीतर चुनाव के परिणामों के प्रति एक किस्म का दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित कर दिया था – हार से हताश और जीत में अतिउत्साही न होने का का गुण. इसके बावजूद 2004 के परिणामों ने मुझ पर पिछली असफलताओं से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डाला..’
इस दार्शनिक दृष्टिकोण ने उनकी आगे की यात्रा जारी रखने में थोड़ी मदद तो की मगर उस समय आडवाणी ये नहीं जानते थे कि उन पर बहुत जल्दी ही इससे भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है. अगले साल ही वे पाकिस्तान की यात्रा पर गए और वहां उन्होंने कराची में मुहम्मद अली जिन्ना की मजार पर उनकी प्रशंसा से भरा एक भाषण दे डाला.
इस बारे में उनकी किताब में जो लिखा है वो एक बार फिर से हमें उस मनोदशा की झलक दे सकता है जिससे अमेरिका की तर्ज पर लड़े गए चुनावी समर में हार के बाद भारतीय राजनीति का ये पुरोधा गुजर रहा होगा. 2005 में उनकी पार्टी खुलेआम उनकी खून की प्यासी हो रही थी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया. ये वही पार्टी थी जिसे अपने खून से सींचा था और अकेले ही 1984 में दो सीटों से 1999 में 182 तक लेके गए थे. जिन्ना विवाद पर उन्होंने लिखा – ‘मेरे पाकिस्तान में रहते ही उथल-पुथल होना शुरू हो गई..इसके बाद की घटनाओं ने पार्टी की एकजुटता पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला और उसके करोड़ों समर्थकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी. इससे मुझे बहुत गहरे और न खत्म होने वाले दर्द का एहसास हुआ. ये निश्चित ही मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख देने वाला समय था, उससे भी ज्यादा दुखदायी जब मुझ पर 1996 में हवाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. उस समय मेरे मन में इसलिए शांति थी क्योंकि मेरी पार्टी दृढ़ता से मेरे साथ खड़ी हुई थी..इसके विपरीत 2005 में मेरी पाकिस्तान यात्रा पर उठे विवाद के दौरान पार्टी के मेरे कई सहयोगियों ने मेरा साथ छोड़ दिया था..’
‘2005 के मध्य में एक दिन मुझसे पार्टी की अध्यक्षता छोड़ देने के लिए कह दिया गया..ये सब मुझे अत्यधिक दुख देने वाला था. मैं दुविधा की स्थिति में था..मेरी दुखद स्थिति ने मुझे कई बार ये सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या मुझे अब शांति से पारिवारिक जीवन का आनंद नहीं उठाना चाहिए..मेरी मानसिक स्थिति अनिश्चितता से जूझ रहे अर्जुन से अलग नही थी. किंतु जब भी मेरे दिमाग में पलायनवादी विचार आते तो मुझे भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता..’
मैं कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी छवि को बदलकर एक उदारवादी, ज्यादा लचीली सोच रखने वाली छवि में तब्दील करना चाहता था
2009 के चुनावों ने आडवाणी को एक बार फिर से उसी स्थिति में ला खड़ा किया है. मगर इस बार कोई भी उनसे ये नहीं कह रहा है कि उन्हें नेता विपक्ष के पद को संभाले रहना चाहिए – उन्हें सिर्फ इसलिए थोड़ा ठहरने के लिए बोला गया है ताकि बिना किसी अंदरूनी झगड़े को दावत दिए आसानी से सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
इसलिए ऐसे में जब आडवाणी अपने भविष्य के बारे में सोचने के साथ-सात अपने चिर-परिचित दार्शनिक दृष्टिकोण से 2009 के चुनावों में पार्टी को मिली पराजय का विश्लेषण करने में लगे हों वे ये भी निर्णय ले सकते हैं कि क्यों न अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में एक अध्याय और जोड़ दिया जाए. अगर 2004 की हार पर लिखे अध्याय का शीर्षक चुनावों में हार, पार्टी में उथल-पुथल था तो इस बार की हार के अध्याय का शीर्षक होगा चुनावों में करारी हार, पार्टी में घमासान. हो सकता है उनकी पार्टी के ही कुछ लोग इसे शायद मैं ये चुनाव क्यों हारा का नाम देना चाहें मगर वह शायद ऐसा लिखा होगा.
‘2004 में चुनावी परिणामों को निर्धारित करने वाला राष्ट्रीय महत्व का कोई अकेला कारक नहीं था. बल्कि कई चीजों ने मिलकर उस समय मतदाताओं को प्रभावित किया था. भारत उदय और ‘फील गुड फैक्टर’ जैसा वाक्यों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया. इस बार पार्टी, संघ परिवार और हमारे गठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने मुझ पर अपना विश्वास जताया और मुझे अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. मुझे, मेरे ऊपर उनके इस विश्वास और इस कार्य की विशालता का एहसास था और मैंने बड़ी विनम्रता से इस चुनौती को स्वीकार करके इस विश्वास पर खरा उतरने के प्रयत्न करने आरंभ कर दिए. मैं चिलचिलाती धूप में बिना थके, बिना रुके एक के बाद एक चुनावी सभाएं करने लगा.
ये देख कर मुझे गहरा दुख होता है कि पिछली बार की 138 सीटों के मुकाबले इस बार भाजपा को लोकसभा की सिर्फ 116 सीटों से ही संतोष करना पड़ा और मुझे पता है कि मेरे कई वरिष्ठ सहयोगी मुझ पर राष्ट्रपति प्रणाली के लोकतंत्र सरीखा चुनावी अभियान चलाने का और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमले करने के आरोप लगा रहे हैं. मगर ये सत्य है कि परमाणु करार के मसले पर अपनी सरकार की बाजी लगाने से पहले के साढ़े चार सालों तक मनमोहन सिंह एक मनोनीत प्रधानमंत्री भर थे जो अपने हर छोटे-बड़े निर्णय के लिए 10 जनपथ की ओर निहारा करते थे. तो अगर मैंने उन्हें कमजोर कह दिया तो इसमें गलत ही क्या है?
बहुतों को मेरा चुनावी अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के जैसा लगा मगर हमारी हार के मूलभूत कारण हमारी देश में भौगौलिक उपस्थिति का सीमित होना है. भाजपा का कई महत्वपूर्ण राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है. चंद्रबाबू नायडू के हमसे विलगाव का कारण भी यही रहा.
पार्टी में गुपचुप ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि मैं उम्र में काफी बड़ा होने के कारण आज के युवा भारत के तौर-तरीकों से सामंजस्य बिठाने के योग्य नहीं हूं. मुझे देश भर से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पत्र और ईमेल मिल रहे हैं जिनमें मेरे प्रति सहानुभूति रखने वाली तरह-तरह की बातें हैं लेकिन ये एक सच्चाई है कि बिना किसी संशय के मतदाता इस बार स्थायी सरकार चाहते थे. वे एक ऐसी सरकार नहीं बनाना चाहते थे जिसमें जरा-जरा सी बात पर भी उठा-पटक होती रहे. इसलिए काफी सोच-विचार के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के 145 से 206 सीटों पर पहुंचने के पीछे मतदाताओं की स्थायित्व की चाह और उसकी पूरे देश में उपस्थिति रही.
मुहम्मद अली जिन्ना पर मेरी टिप्पणी पर पार्टी में जो उथल-पुथल मची उसका जिक्र मैंने अपनी जिंदगी के सबसे दुखद समय के रूप में किया है. मेरे खुद के सहयोगियों ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया. मगर वे उस समय ये समझने में असफल रहे कि भाजपा के लिए मेरी उस टिप्पणी का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व था. मैं इसे, राम मंदिर अभियान के बाद के दौर में अपनी हार से तारतम्य बिठाने के लिए जद्दोजहद करती एक पार्टी के जीवन में बदलाव का मोड़ बनाना चाहता था.
उस समय तक ये साफ हो चुका था कि वाजपेयीजी अब सिर्फ हमारे संरक्षक और दिग्दर्शक का काम करने वाले हैं और ऐसी स्थिति में मुझे और पार्टी को एक नयी छवि की आवश्यकता है, एक ऐसी छवि जो आज के भारत से मेल खाती हो. मैं कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी छवि को बदलकर एक उदारवादी, ज्यादा लचीली सोच रखने वाली छवि में तब्दील करना चाहता था. पार्टी में किसी को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी कि वाजपेयी जी स्वभावत: अपने में ही और अपने परिवार के साथ खामोशी में समय बिताने और अकेले में कविताएं लिखने के शौकीन थे. मगर मैं ये जानकर हैरान हूं कि मेरे सहयोगी आज ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी की कीमत पर अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता था. और ये भी कि मेरे कुछ विश्वस्त साथियों ने सुधींद्र कुलकर्णी के नेतृत्व में मेरे लिए एक समानांतर प्रचार अभियान चलाया जबकि इसके लिए पहले से मेरे सहयोगी अरुण जेतली के नेतृत्व वाली अभियान कमेटी मौजूद थी. आलोचना इस बात की हो रही है कि मैंने कुलकर्णी की टीम, जिसमें ब्लॉगर्स, तकनीकी विशेषज्ञ और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स शामिल थे, की ज्यादा सुनी. मगर यहां विरोधाभास साफ झलकता है. मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं आज के भारत से तालमेल बिठाने के योग्य नहीं हूं और यहां मेरी उसी भारत के नुमाइंदों का साथ देने और लेने के लिए आलोचना की जा रही है.
पिछली साल के विधानसभा चुनावों में दिल्ली और राजस्थान में मिली हार के बाद पूरी पार्टी को बैठकर गंभीर विचार-विमर्श करना चाहिए था. ये सच है कि मुंबई पर हुए आतंकी हमलों से पहले हम प्रगति की राह पर अग्रसर थे. इसके बाद आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया और जहां हम आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दे रहे थे वहीं लोग अब स्थायित्व की चाह रखने लगे थे.
2005 के विपरीत, जब मेरी मानसिक स्थिति अनिश्चितता से जूझ रहे अर्जुन से अलग नही थी, इस बार मैंने तुरंत ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया. मगर पार्टी में खींचतान के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है.
मुझे नेता विपक्ष बनने से बिल्कुल ही इनकार कर देना चाहिए या अपने सहयोगियों की बात मान कर इस पद को स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं इस बात को लेकर दुविधा में हूं. मुझे इस तरह के पदों के साथ मिलने वाले लाभों और ताकत ने कभी इतना आकर्षित नहीं किया. मैं जल्दी ही ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूंगा.’