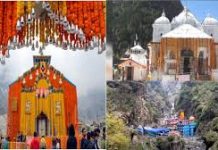संगीत जो अपनी सच्चाई खुद बना और नष्ट कर रहा है. बाहर की सच्चाई की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा करता हुआ, उससे उदासीन. संगीत के अपने उजास में झिलमिलाते-जगमगाते चेहरे. जो दुनिया गिनती करती, हिसाब लगाती है उसे हाशिए पर करता अपनी परंपरा को पुनर्नवा करता, एकत्र करता, सबको संग-साथ में गूंथता संगीत. आवाज जो पास लाती है – आवाज जो पुकारती है, दुलार से, मनुहार से, इसरार से. आवाज जो अपना स्थापत्य रचती है और घेरते-रचते उसे ओझल भी करती जाती है. आवाज जो दिलासा देती है, जो भरोसा दिलाती है कि हम, कुछ देर के लिए, पल-पल नजदीक आती अपनी नश्वरता से छुटकारा पा सकते हैं. आवाज जो सिर्फ आदमी की है और दूसरों को संबोधित होते हुए भी अपने आप में भरी-पूरी है.
आतंक, हिंसा, हत्या और धमाके से भरे वर्ष से क्या इस तरह छुटकारा पाया जा सकता है? शायद नहीं, बहुत देर के लिए तो नहीं ही. लेकिन क्या यह भूला जा सकता है कि दुनिया में हो रहे निरंतर विनाश के विरुद्ध सृजन ही एकमात्र संभव प्रतिरोध, बचाव है? हम बच नहीं सकते लेकिन कुछ न कुछ बचा सकते हैं. हमारे कठिन और हिंसक समय में जो बचा नहीं सकता वह आदमी नहीं कहा सकता. इस समझ को धूमिल नहीं पड़ना चाहिए कि कलाएं सच्चाई से भगोड़ों की पनाहगाह नहीं बल्कि दूसरी सच्चाई की जगह हैं. वह सच्चाई भी हमारी रोजमर्रा की सच्चाई की ही तरह मटमैली है, उसमें भी और आशंकाओं का संसार है. हम यह अक्सर भूल जाते हैं कि कोई भी समय बहुत-सी सच्चाइयों में फंसा-बसा समय होता है. मनुष्य का सच न कभी एक है, न उसकी सच्चाई इकहरी है.
एक सुखद विडंबना यह है कि मीडिया द्वारा मनोरंजन, फैशन, अपराध और राजनीति के अत्याकर्षण और दबाव में शास्त्रीय कलाओं की लगातार उपेक्षा के बावजूद, उनमें सर्जनात्मक, गतिशीलता और कल्पनाशील साहस की कोई कटौती नहीं हुई है. विशेषत: शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में लगातार युवा प्रतिभाएं उभर और अपना स्थान बना रही हैं. उनमें से कई अपने-अपने घरानों या शैलियों की विशिष्टता को कायम रखने की कोशिश करके शास्त्रीय संगीत की बहुलता को नया जीवन दे रही हैं. कुछ ऐसी हैं जो निर्भीक प्रयोग करने से घबराती नहीं हैं. नायक-छवियों से आक्रांत समय में ऐसी कोशिशों को समय रहते रसिकता और पोषण का समर्थन नहीं मिल पाएगा, यह आशंका जागती है.कलाकर्म आर्थिक रूप से अब एक अच्छा व्यवसाय बन गया है. बल्कि एक समय साथ रहनेवाले ‘दरिद्रता में सहचर’ कला और साहित्य, इस वजह से, काफी दूर हो गए हैं
शास्त्रीय नृत्य में एकल प्रदर्शन थोड़ा उतार पर है जो कि दुर्भाग्य की बात है. इस वर्ष न्यूयॉर्क, बैंकाक से लेकर दिल्ली आदि में समूह-नृत्य प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति, जिसे पर्याप्त वित्तीय और संस्थागत समर्थन मिला हुआ है, नृत्य की शास्त्रीयता और सर्जनात्मकता या कि समकालीनता में कोई इजाफा कर पायी है इसमें संदेह है. आशा, फिर भी, इस तथ्य से बंधती है कि सामूहिकता के प्रबल आकर्षण और प्रलोभन के बावजूद कई शैलियों में ऐसे युवा नृत्यकार हैं जो निजता और अद्वितीयता की साधना कर पा रहे हैं. ऐसे भी कुछ हैं, भले अपवाद ही, जो अपनी शास्त्रीय शैली को ही विस्तार देते हुए उसमें समकालीन अभिप्रायों को समाहित कर पा रहे हैं. यह प्रमाण है कि शास्त्रीयता में समकालीनता की पूरी संभावना है और दोनों के बीच सर्जनात्मक द्वंद्व से शास्त्रीयता का विस्तार होता है और समकालीनता भी शास्त्रीयता के अहाते में आ जाती है.
शास्त्रीय संगीत के वर्तमान और भविष्य को लेकर कुछ शीर्षस्थ कलाकार चिंतित हुए हैं और उन्होंने एक अनौपचारिक संगठन बनाया है जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैलियों के कई मूर्धन्य शामिल हैं. उद्योगपतियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि से संवाद कर शास्त्रीय संगीत के लिए अधिक संवेदनशील सुविधाएं और माहौल बनाने के लिए की गई इस पहल का महत्व है. अलग से एक कोशिश यह भी हो रही है कि सार्वजनिक उद्योगों को अपने-अपने क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत और नृत्य में गुरु-शिष्य परंपरा के आधार पर नए शिष्यों को दीक्षित करने के एक देशव्यापी अभियान में शामिल किया जाए, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत.
संगीत और नृत्य दोनों को ही, दुर्भाग्य से, गंभीर और उत्तरदायी आलोचना नहीं मिल पाई है. इस वर्ष इस दुखद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. अगर यही हालत बनी रही तो इन कलाओं के सत्व के क्षरण का खतरा हो सकता है. सजग आलोचना सक्रिय सृजन के लिए जरूरी है. स्वयं संगीतकारों द्वारा इस तरह का आलोचनात्मक माहौल बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है. उल्टे कई वरिष्ठ संगीतकारों का संतान-प्रेम इस कदर प्रबल है कि वे पूरी बेशर्मी से अपने बच्चों को सार्वजनिक मान्यता दिलवाने में मुब्तला हैं. यह दूसरी बात है कि इन चिकने-चुपड़े और अक्सर मीडिया द्वारा अनर्जित प्रशंसा पाए संगीतकारों में किसी को भी वह दर्जा नहीं दिया जा सकता जो सांगली, बेलगाम, धारवाड़ आदि के युवा संगीतकारों ने बिना किसी सिफारिश या समर्थन के, बिना किसी ‘माई-बाप’ के निर्लज्ज समर्थन के अपने दम पर हासिल किया है. अगर राजनीति में संतान-प्रेम कहर ढाता है तो संगीत में वह भला कैसे कुछ और कर सकता है?
आशा यह है कि सो युवा संगीतकारों पर ध्यान जाएगा और उन्हें वह समर्थन मिलेगा, संस्थाओं और रसिकों से जिसके कि वे सर्वथा सुपात्र हैं. आशंका यह है कि चूंकि मूर्धन्यों का दबाव कम नहीं होनेवाला, उनकी कमजोर संतानें सब जस और सुविधाएं बटोर लेंगी.
क्या हम एक अतिरंजित स्थिति से सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं? क्या कला में कीमत के आतंक के बरक्स फिर से मूल्य का वर्चस्व स्थापित हो रहा है? ये कुछ सवाल हैं जो ललित कला की दुनिया में इस वक्त तीखेपन के साथ उठ रहे हैं. सच ये है कि पिछले दो-तीन बरसों में कला में छवि काम से कम कीमत से ज्यादा बनने लगी थी.
इसका प्रतितर्क था कि काम में दम है तभी न कीमत ज्यादा मिल रही है. भारतीय आधुनिक कला को देर से सही इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय दुनिया और बाजार में कुछ जगह मिलना शुरू हुई. स्वयं भारत में कला का व्यापार तेजी से बढ़ा, भले वह अभी वहीं नहीं पहुंचा है जहां आधुनिकता में शायद हमसे बाद में आनेवाली चीनी आधुनिक कला पहुंच गई है. साधनहीनता में काफी वक्त गुजारने की कलाकारों की मजबूरी अब काफी घट गई है. कलाकर्म आर्थिक रूप से अब एक अच्छा व्यवसाय बन गया है. बल्कि एक समय साथ रहनेवाले ‘दरिद्रता में सहचर’ कला और साहित्य, इस वजह से, काफी दूर हो गए हैं. कला में पैसा है, साहित्य उसका गरीब बिरादर ही है और आगे भी बना रहेगा.
आर्थिक मंदी का प्रभाव कला के बाजार पर भी पड़ा है. कला-दीर्घाओं में बिक्री घट गई है और नए काम को आक्रामक ढंग से पेश करने की जोखिम-उठाऊ वृत्ति कुछ कमजोर पड़ी है. पर यह सच्चाई फिर भी अपनी जगह है कि इस समय युवा प्रतिभा का सबसे सर्जनात्मक, दुस्साहसी और निर्भीक विस्फोट ललित कला में ही है. इतने अधिक प्रतिभासंपन्न युवा न तो किसी अन्य कला में हैं और न ही इसके पहले शायद ललित कला में ही हुए हैं. इन दिनों हर दिन डाक में कहीं से, दूर-दराज से, एक कैटलाग जरूर आता है. इससे आशा बंधती है. इससे भी कि कला का अभिलेखन बेहतर हुआ है. लेकिन विडंबना यह है कि कला की आलोचना का क्षेत्र उतनी तेजी से विकसित और विस्तृत नहीं हो पा रहा है. कला की, विशेषकर प्रयोगधर्मी और सरहदों का अतिक्रमण करने वाली कला की सामाजिक मान्यता भी बढ़ी है पर आलोचनात्मक विश्लेषण और आकलन का, मूल्यांकन का उसके बराबर विकास और विस्तार नहीं हुआ है. कई बार यह आशंका होती है कि मूल्यांकन का काम भी कहीं बाजारू न हो जाए. तब ऐसी कला भी बढ़ जाएगी जो दाम से उत्साहित होगी, मूल्य से प्रेरित नहीं.
आम तौर पर साहित्य के मुकाबले अन्य कलाओं में अपने समय से सीधे जुड़ने और सीधे नागरिक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति कुछ शिथिल ही रही है. कहा जाता है कि वे समय की राजनीति में कम, अनंत की राजनीति में अधिक भरोसा रखते हैं. लेकिन हमारा समय ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग-थलग रहने की सुविधा दे.
शायद यह सामान्यीकरण उचित नहीं है कि ऐसे हस्तक्षेप से कलाएं दूर हैं. उनका हस्तक्षेप प्राय: अधिक सूक्ष्म होने से अलक्षित हो जाता है. आशा है कि देर-सबेर ऐसे औजार हमारे पास होंगें जो हमारी समझ बढ़ाएंगे. आशंका यह है कि ऐसे औजारों को भोंथरे करने के लिए बाजार, मीडिया और लोकप्रियता की शक्तियां सक्रिय रहेंगी. हम आशा और आशंका के बीच के उजास में हैं. कुहरा है, छंटता और बढ़ता, बढ़ता और छंटता.
अशोक वाजपेयी