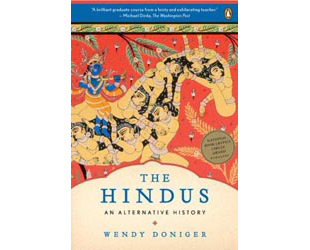विचार का जवाब विचार होना चाहिए या कानूनी प्रतिबंध या फिर हिंसा, इस सवाल पर फिर से बहस छिड़ गई है. इस बार इसकी वजह बना है प्रकाशक द्वारा एक विवादित किताब को बाजार से वापस लेने और नष्ट करने का फैसला. पेंगुइन इंडिया ने यह निर्णय अमेरिकी लेखिका वेंडी डॉनिगर की किताब ‘द हिंदूज़: ऐन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री’ पर लिया है. यह किताब 2009 में प्रकाशित हुई थी. दरअसल शिक्षा बचाओ आंदोलन नाम के एक संगठन ने 2011 में पेंगुइन इंडिया के खिलाफ मामला दायर किया था. उसका कहना था कि कि इस किताब में कई पूर्वाग्रह और तथ्यात्मक गलतियां हैं और यह हिंदुओं का अपमान करती है. पेंगुइन इंडिया इस पुस्तक को वापस लेने और उसकी बची प्रतियों को नष्ट करने पर सहमत हो गई और मामला निपट गया.

1940 में न्यूयॉर्क में जम्मी डॉनिगर को भारतीय संस्कृति की गहरी अध्येता माना जाता है. फिलहाल वे शिकागो विश्वविद्यालय में धर्मों के इतिहास विषय की प्रोफेसर हैं. वे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अंतरराष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड में भी हैं. उनकी इस किताब को दो साल पहले प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका पुरस्कार भी मिल चुका है. शिक्षा बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष दीना नाथ बत्रा का आरोप है कि उनकी यह किताब ‘सेक्स और कामुकता’ पर आधारित है. उनका कहना है कि किताब के मुख्य पृष्ठ पर छपी तस्वीर तो आपत्तिजनक है ही, साथ ही किताब में देवी देवताओं और महापुरुषों के बारे में भी ओछी टिप्पणियां की गई हैं. इससे पूरे समाज की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है.
उधर, वेंडी डोनिगर ने फैसले पर अफ़सोस जताया है. बीबीसी से बातचीत में उनका कहना था कि उन्हें इस बात की आशंका थी. हालांकि जिस तरह से भारत और पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया हुई उस पर वे चकित भी थीं. उन्होंने कानून बदलने की जरूरत भी बताई. डोनिगर का कहना था, “कानून काफी क्रूर है. किसी हिंदू को आहत करने वाली किताब के प्रकाशक को ये अपराधी साबित करता है.” किताब हिंदुओं के लिए अपमानजक है, इस आरोप पर उनका कहना था, ” बहुत से हिंदुओं को किताब काफी अच्छी लगी और उन्होंने इस बारे में मुझे लिखा भी है. किताब काफी बिकी भी है. इसलिए ऐसा नहीं है कि किताब बस हिंदू विरोधी है.
दरअसल तो ये काफ़ी हिंदू समर्थक किताब है. ये कुछ ख़ास तरह के हिंदुओं को बुरी लगेगी. दक्षिणपंथी हिंदुओं को, कट्टरपंथी हिंदुओं को और ऐसे लोगों को जो किताब को दबाना चाहते हैं.”
इस मामले की बौद्धिक समाज में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है. अपने एक लेख में चर्चित इतिहास रामचंद्र गुहा कहते हैं, ‘डॉनिगर का मामला सबसे ताजा उदाहरण है कि अदालतें, प्रकाशक और राजनेता बौद्धिक आजादी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे.’ जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है. उनके मुताबिक दीनानाथ बत्रा पूरे समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं. एक समाचार वेबसाइट से बातचीत में वे कहते हैं कि जिसे नहीं पढ़ना है वह न पढ़े, लेकिन प्रतिबंध या रोक अच्छी बात नहीं है.”
भारत में सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी आलोचना देखी जा रही है. कई लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लग रही इन पाबंदियों पर चिंतित हैं. हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जिसका मानना है कि धार्मिक भावनाओं को ख्याल रखना भी जरूरी है.
बीबीसी से बातचीत में साहित्यकार उमा वासुदेव कहती हैं कि वे किताबों पर किसी तरह के प्रतिबंध के पक्ष में तो नहीं हैं, लेकिन लेखकों को भी चाहिए कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं.
उधर, पेंगुइन इंडिया का तर्क है कि दूसरों की तरह वह भी देश के कानून का पालन करने को बाध्य है. अपने बयान में उसने कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में आपराधिक धाराओं के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनकी वजह से कानून तोड़े बगैर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचाए रखना मुश्किल है. प्रकाशक का कहना था, “हम समझते हैं कि इसकी वजह से भारत में किसी भी प्रकाशक के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर बनाकर रखना मुश्किल होगा.”
किताबों पर विवाद भारत में नया नहीं है. कई लोग मानते हैं कि इस मुद्दे पर पहली और बुनियादी गलती 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने की थी. तब उन्होंने सलमान रश्दी की किताब द सेटेनिक वर्सेस को यह कहकर प्रतिबंधित कर दिया था कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं. भारत ने ईरान और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों से भी पहले यह काम कर दिया था. उस समय इतिहासकार धर्म कुमार ने लिखा कि यह प्रतिबंध सरकार की कमजोरी का संकेत है. किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में ईशनिंदा की भी जगह होनी चाहिए. भारत के राष्ट्रपति किसी धर्म या सारे धर्मों के रक्षक नहीं हैं.
एक वर्ग मानता है कि राजीव गांधी के इस कमजोर कदम ने हर तरह के कट्टरपंथियों की हिम्मत बढ़ा दी. बाद के दिनों में महाराष्ट्र में जेम्स लेन की शिवाजी पर लिखी किताब को भी निशाना बनाया गया. ऐसा करने वालों ने राज्य सरकार को किताब पर प्रतिबंध लगाने के लिेए मजबूर कर दिया. सरकार के प्रतिबंध को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था लेकिन ऑक्सफोर्ड प्रेस फिर भी किताब बेचने को लेकर डरी हुई थी. उसे लग रहा था कि उसके दफ्तर पर गुंडे हमला करेंगे और पुलिस सिर्फ देखती रहेगी. जोसेफ लेलेवेल्ड की किताब पर भी भारत में 2011 में हंगामा हो चुका है, जिसमें दावा किया गया था कि महात्मा गांधी समलैंगिक थे. गुजरात सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है.
अपने लेख में रामचंद्र गुहा कहते हैं, ‘यह बड़ी दुखद बात है. कुछ साल पहले मेरे प्रकाशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी निचली अदालत में याचिकाकर्ता से अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया था और के रामानुजन द्वारा लिखा गया एक निबंध वापस ले लिया था.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘डॉनिगर और रामानुजन उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बहुत गहराई से अध्ययन किया है. उन्होंने अपने बारे में हमारी समझ को और समृद्ध किया है. हिंदू धर्म के ठेकेदार होने का दावा करने वाले चंद संकीर्ण सोच वाले लोग अगर ऐसे शोधपूर्ण और सार्थक काम को प्रतिबंधित करवा देते हैं तो यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं.’
एक वर्ग का मानना है कि बड़े प्रकाशकों को इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने चाहिए. पेंगुइन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दोनों ही बड़े प्रकाशक हैं. उनके पास लड़ने के लिए संसाधन भी हैं. जैसा कि गुहा कहते हैं, ‘उम्मीद करना स्वाभाविक ही था कि वे अपनी लड़ाई लड़ेंगे. ऊपरी अदालतों तक जाएंगे. ताकि उनके प्रतिष्ठित लेखकों की स्वतंत्रता का अधिकार सलामत रहे. आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया.’
जानी-मानी लेखिका अरुंधती राय भी एक लेख में कहती हैं, ‘आप क्यों डर गए? क्या आप भूल गए आप कौन हैं? आप दुनिया के सबसे पुराने और बड़े प्रकाशकों में से हैं. आपने इतिहास के कुछ सबसे बड़े लेखकों को प्रकाशित किया है. आप प्रकाशक का धर्म निभाते हुए हमेशा लेखकों के साथ खड़े रहे हैं, हिंसा और विषमता के बावजूद अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ लड़े हैं. और अभी तो कोई फतवा प्रतिबंध या अदालती आदेश भी नहीं था. अदालत के बाहर चुपचाप दूसरे पक्ष से समझौता करके आपने खुद को ही शर्मसार किया. आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सारे साधन थे. आपको जवाब देना होगा. कम से कम अपने लेखकों को तो आपको जवाब देना ही चाहिए.’
कई जानकार मानते हैं कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनकी मंशा नुकसान को कम से कम रखने की रही होगी. फैसले के बाद पेंगुइन का बयान भी आया कि अपने कर्मचारियों को धमकियों और प्रताड़ना से बचाने की उसकी नैतिक जिम्मेदारी है. कुछ के मुताबिक प्रकाशक के इतनी जल्दी हथियार डालने की एक वजह यह भी हो सकती है कि डॉनिगर और रामानुजन दोनों का ही ताल्लुक अमेरिकी विश्वविद्यालयों से जुड़ता है. जैसा कि गुहा कहते हैं, ‘अगर वे भारतीय विद्वान होते तो इस पर उठा हंगामा शायद प्रकाशकों पर दबाव बना देता कि वे अपनी लड़ाई लड़ें.’
गुहा यह भी मानते हैं कि उनके ऐसा न करने का तीसरा और शायद सबसे अहम कारण यह हो सकता है कि भारत सरकार और राज्यों की सरकारें भी वास्तव में बौद्धिक स्वतंत्रता में यकीन नहीं करतीं. वे कहते हैं, ‘अलग-अलग पार्टियों के नेता ही कई बार यह जाहिर कर चुके हैं कि किताबों पर प्रतिबंध लगाने और लेखकों को परेशान करने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.’
इस मामले में हर पार्टी का दामन दागदार है. यहां तक कि वामपंथियों का भी. अपने उपन्यास लज्जा के चलते मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आने के बाद बांग्लादेश से निर्वासित तसलीमा पश्चिम बंगाल में रहना चाहती थीं. यहां वे सांस्कृतिक रूप से सहज महसूस करती थीं. लेकिन 2007 में वहां कट्टरपंथियों के बवाल के बाद वाम मोर्चा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि वह कोलकाता में उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती. मजबूरन उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ी. मकबूल फिदा हुसैन का भी उदाहरण है जो डॉनिगर और रामानुजन से पहले हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आए थे. उनका काम दर्शाती प्रदर्शनियों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं. फिर एक अभियान के तहत अलग-अलग जगहों में उनके खिलाफ कई मामले दायर कर दिए गए. हताशा में उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा.
अब सवाल यह है कि इस शोषण और प्रताड़ना को खत्म कैसे किया जाए. गुहा लिखते हैं, ‘एक उपाय तो यह हो सकता है कि निचली अदालतें धड़ाधड़ ऐसे मामलों को स्वीकार ही न करें जिनकी नीयत ही विवाद पैदा करना हो. दूसरा यह है कि प्रकाशक भी थोड़ी हिम्मत दिखाएं. डरे नहीं. और सबसे ज्यादा मदद इस बात से होगी कि देश का राजनीतिक वर्ग यह संदेश दे कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के जो आदर्श हैं उन्हें वह खंडित नहीं होने देगा.’
तीनों ही चीजों की उम्मीद नहीं लगती. गुहा मानते हैं कि सरकार में साहस के साथ-साथ दूरदृष्टि की भी कमी है. वे कहते हैं, ‘आगे के लिए भी आसार ठीक नहीं लगते.’ अरुंधती कहती हैं, ‘चुनाव होने में भी कुछ महीने हैं. फासीवादी ताकतें अभी चुनाव प्रचार कर रही हैं. माहौल उनके पक्ष में भी दिख रहा है. लेकिन अभी वे सत्ता में तो नहीं हैं और आप अभी से झुक गए. इसका हम क्या अर्थ निकालें. क्या अब हमें ऐसी किताबें लिखनी होंगी, जिनमें हिंदुत्व की जरा भी आलोचना न हो. या फिर हमें जोखिम के लिए तैयार रहें कि हमारी किताबें बिकेंगी नहीं.’
तो फिर आगे क्या हो? अपने एक लेख में दिवंगत पत्रकार प्रभाष जोशी कहते हैं कि एक समय जब भारत में बौद्ध धर्म प्रधान हो गया था तो सनातन धर्म का प्रचार करने निकले शंकराचार्य अपने साथ उपद्रवियों का झुंड लेकर नहीं चले थे. पूरा भारत घूमकर उन्होंने सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से अपने धर्म को पुनर्जीवन दे दिया था.
दूसरा उदाहरण अमेरिकी लेखिका कैथरीन मायो की चर्चित किताब मदरइंडिया का है. 1927 में आई और उस दौर की सबसे चर्चित और बिकने वाली कृतियों में रही इस किताब में भारत को मानव सभ्यता के शरीर में मौजूद एक ट्यूमर बताया गया था. मायो का कहना था कि अगर जल्द ही इसका इलाज नहीं किया गया तो जल्द ही सारी दुनिया इससे होने वाली प्राणघातक महामारियों की चपेट में आ जाएगी. उनका यह भी तर्क था कि ब्रिटिश राज ही दुनिया को इस ट्यूमर से होने वाले नुकसान से बचा सकता है इसलिए भारत की आजादी की मांग बेतुकी है.
मदरइंडिया का भारत में भारी विरोध हुआ. किताब के साथ मायो के पुतले भी जलाए गए. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किताब के विरोध में 50 से भी ज्यादा किताबें और पर्चे छपे. सोशल नेटवर्किंग साइट टिवटर पर अपनी एक टिप्पणी में रामचंद्र गुहा लिखते भी हैं, “अगर किसी को कोई किताब पसंद नहीं आती है तो उसका जवाब है एक और किताब न कि उस पर प्रतिबंध या कानूनी कार्रवाई या फिर मार-पिटाई की धमकी.”