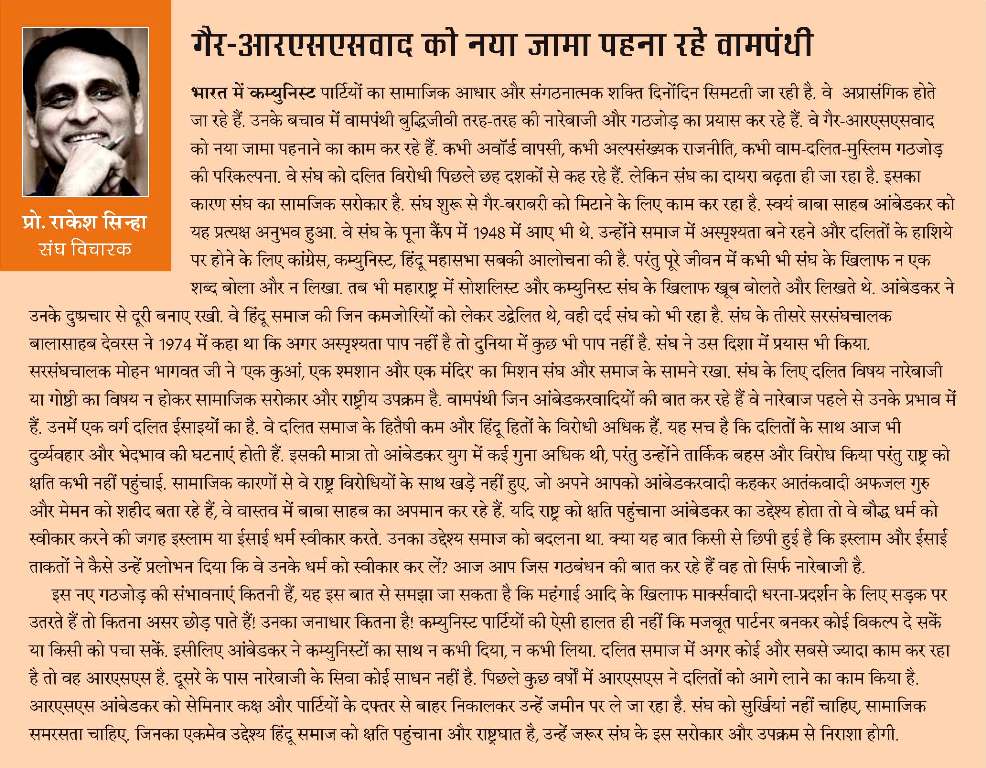जेएनयू में कथित देशविरोधी नारे को लेकर बवाल हुआ तो छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी से पहले उनके भाषण में ‘जय भीम, लाल सलाम’ का नारा शामिल था. उन्होंने अपने भाषण में कहा, ‘जब हम महिलाओं के हक की बात करते हैं तो ये (संघ-भाजपा के लोग) कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हो. हम बर्बाद करना चाहते हैं शोषण की संस्कृति को, जातिवाद की संस्कृति को, मनुवाद और ब्राह्मणवाद की संस्कृति को. आपकी संस्कृति की परिभाषा से हमारी संस्कृति की परिभाषा तय नहीं होगी. इनको दिक्कत होती है जब इस मुल्क के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब लोग लाल सलाम के साथ नीला सलाम का नारा लगाते हैं.’ उन्होंने भाषण खत्म किया तो ‘इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम’ नारा लगाया. कन्हैया जेल से छूटे तो भी उनके भाषण में ‘लाल और नीले’ झंडे की एकजुटता का संदेश प्रमुखता से मौजूद था. इसके पहले हैदराबाद में रोहित वेमुला प्रकरण में भी यह नारा गूंज रहा था. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों में घटी घटनाओं के बाद आंबेडकरवादी और मार्क्सवादी संगठनों की नजदीकी पर चर्चा जोर पकड़ रही है.
सत्ता में आने के बाद भाजपा ने लगभग सभी इतिहास-पुरुषों पर अपनी दावेदारी पेश की. इसकी शुरुआत सरदार पटेल से हुई थी और फिर इस कड़ी में गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आंबेडकर आदि एक-एक कर जुड़ते गए. 14 अप्रैल को देश भर में आंबेडकर की 125वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने भव्य आयोजन किए. इस दिन सोशल मीडिया पर भी आंबेडकर खूब सेलिब्रेट किए गए. इस सेलिब्रेशन में यह सवाल शामिल था कि ‘जय भीम और लाल सलाम’ की भविष्य की संभावनाएं क्या हैं.
आईआईएम इंदौर के शोधछात्र विनोद कुमार कहते हैं, ‘भारत में वामपंथियों की गलती यही थी कि वे इस देश में गरीबी की सबसे बड़ी वजह और हकीकत ‘जाति’ को उपेक्षित करते रहे (और इसी का फल भुगता है). अब अगर नई पीढ़ी समझ रही है, बदल रही है तो स्वागत कीजिए. पुरानी पीढ़ी के आधार पर हर पीढ़ी पर संदेह करना ही तो मनुवादी सोच है, हमें इसी से लड़ना है. खुद पर भरोसा रखिए. अगर इस देश के मनुवाद से लड़ना है तो सारी गैरमनुवादी ताकतों को एकजुट होना होगा; हमारी ताकत अपने हित को समझने में, हमारी समझ में होगी हमारे संदेह में नहीं. भारत में वामपंथ का मार्ग सही मायने में आंबेडकर की तरफ बढ़े बिना हासिल नहीं होगा.’
[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
आंबेडकरवाद और मार्क्सवाद की सिंथेसिस की जरूरत है : अशोक कुमार पांडेय
वामपंथ और दलित राजनीति के बीच एक तरह का अंतः संबंध शुरू से रहा ही है. वाम आंदोलन सर्वहारा का पक्षधर है और इस देश के सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से आता है, जो भूमिहीन है, कृषि मजदूर है और शहरी समाज के सबसे निचले तबके की नौकरियों में शोषण का शिकार है. आंबेडकर के समय से ही दोनों आंदोलनों को करीब लाने की कोशिशें हुईं, संवाद भी हुए लेकिन अगर एका नहीं बन सका तो उसके लिए दोनों के साथ-साथ तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं. वाम आंदोलन में शामिल कई तत्व जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति नहीं पा सके थे, पार्टी संवैधानिक और गैर-संवैधानिक तरीकों से इंकलाब की राहों को लेकर एक दिग्भ्रम जैसी स्थिति में रही और डॉ. आंबेडकर संविधान को लेकर आशान्वित थे, उनके नजरिये में यह दलित समुदाय को उसके अधिकार दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया था. बाद में नामदेव ढसाल जैसे विद्रोही दलित कवि ने मार्क्सवाद और आंबेडकरवाद की एक सिंथेसिस करने की कोशिश की. राव साहब कसबे की किताब ‘मार्क्स और आंबेडकर’ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी, लेकिन अलग-अलग वजहों से कोई ठोस पहल नहीं हो पाई. कम्युनिस्ट पार्टियां वर्ग की अपनी आर्थिक समझ को भारतीय परिस्थितियों में जाति से नहीं जोड़ पाईं, हालांकि दलितों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर पार्टियों की पक्षधरता हमेशा साफ रही. बिहार, झारखंड, ओडिशा सहित जिन जगहों पर सीधे किसान संघर्ष चले, वहां भूमिहीन दलितों की एक बड़ी संख्या जुड़ी भी. दलित राजनीति भी रामदास अठावले से मायावती तक तमाम मोड़ पार करती रही. कभी उत्तर प्रदेश में भाजपा से गठबंधन हुआ, कभी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ दोस्ती हुई. हिंदू राष्ट्र को दलितों के लिए सबसे खतरनाक बताने वाले डॉ. आंबेडकर के अनुयायियों के लिए यह विचलन सहज तो नहीं ही था.
आज के समय वामपंथ और आंबेडकरवाद के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं- आवारा पूंजी व जल-जंगल-जमीन की लूट और दक्षिणपंथी फासीवाद का उदय. रोहित वेमुला के साथ प्रशासन का व्यवहार और उसकी आत्महत्या इस संकट को बहुत स्पष्टतः व्यंजित करती है. जाति और आर्थिक वंचना का दंश साथ मिलकर इस संकट को इतना गहरा कर देता है कि संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता. इसलिए लाल और नीले का साथ आना कोई चुनावी गठबंधन या सत्ता का खेल नहीं, देश की वंचित-दमित जनता की मुक्ति का सवाल है. यह ऐतिहासिक आवश्यकता है कि आंबेडकरवाद और मार्क्सवाद की एक ऐसी सिंथेसिस प्रस्तुत की जाए जो भारत में मुक्ति के एक लंबे और फैसलाकुन संघर्ष के लिए आवश्यक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के लिए वैचारिक आधार दे सके. आज लेखकों-बुद्धिजीवियों और छात्रों के बीच इसे लेकर एक सहमति-सी बनती दिख रही है, देखना यह होगा कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इसे कितनी गंभीरता से लेता है. आज अगर वह इस ऐतिहासिक मौके को चूकता है तो यह दोनों आंदोलनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा.[/symple_box]
भागलपुर के एक कॉलेज में अध्यापक डॉ. योगेंद्र ने फेसबुक पर लिखा, ‘मैं इंतजार कर रहा हूं कि नीला और लाल कब और कहां मिल रहे हैं. जेल से लौटने के बाद जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया ने बयान दिया था. इससे नीला-लाल की बहस जोर पकड़ ली है. लाल के बड़े-बड़े नेता चुप मारे हुए हैं. लगता है कि ऐसा होने पर उनकी कुर्सी को खतरा है. यह सर्वेक्षण मजेदार होगा कि लाल के मौजूदा नेतृत्व में नीला कितना प्रतिशत है?’
इस बहस ने शायद आरएसएस-भाजपा को असहज स्थिति में ला दिया है क्योंकि दलितों और पिछड़ों का मार्क्सवादियों के साथ जाना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है. आंबेडकर जयंती पर आरएसएस के मुखपत्र ‘पाञ्चजन्य’ और ‘ऑर्गनाइजर’ ने मार्क्स और आंबेडकर को साथ जोड़ने को ‘कुत्सित कृत्य’ बताकर उसकी कड़ी आलोचना भी कर डाली है.
इस नए समीकरण की चर्चा कैंपसों से बाहर लेखक समुदाय में भी है. रोहित वेमुला प्रकरण के बाद दिल्ली में पांच लेखक संगठनों ने ‘आजाद वतन, आजाद जुबान’ नाम से एक आयोजन शुरू किया है. यह आयोजन आंबेडकर की 125वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भी गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली में संपन्न हुआ. यह अपने आप में ऐतिहासिक है कि इन पांच संगठनों में तीन वामपंथी संगठन- ‘जनवादी लेखक संघ’, ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ और ‘जन संस्कृति मंच’ हैं और दो दलित संगठन- ‘दलित लेखक संघ’ और ‘साहित्य संवाद’. इन संगठनों का कहना है, ‘भाजपा का हिंदूवादी राष्ट्रवाद प्रगतिशील, समाजवादी और दलित तबकों के लिए खतरा है जिससे मिलकर लड़ना ही कारगर उपाय हो सकता है.’
इस कार्यक्रम में शरीक हुए जेएनयू छात्रसंघ महासचिव रामा नागा ने कहा, ‘सवाल यह नहीं है कि हमारे झंडे का रंग लाल है या नीला, सवाल यह है कि इन दोनों को मिलकर भगवा से लड़ना है. जिस तरह से हम पर हमले बढ़े हैं, हम साथ आने को मजबूर हुए हैं. सवाल लाल-नीले के विलय या एक हो जाने का नहीं, सवाल साथ मिलकर फासीवाद से लड़ने का है.’
आंबेडकरवाद और मार्क्सवाद के साथ आने की इस नई परिघटना पर जेएनयू के शोधछात्र ताराशंकर कहते हैं, ‘मेरा मानना है कि चूंकि एक बड़ी लड़ाई है पूंजीवाद के खिलाफ, जो आर्थिक गैर-बराबरी का मसला है, और जो तमाम तरह की गैर-बराबरी को जन्म देता है, उस बड़ी गैर-बराबरी के समानांतर इस तरह की हजारों लड़ाइयां हमें लड़नी होती हैं. जैसे कि जेंडर का मसला हो, जाति का मसला हो, छुआछूत का मसला हो, आजादी हो. इस तरह की तमाम समानांतर लड़ाइयां लड़नी होती हैं. चूंकि मार्क्सवाद एक जगह थोड़ा-सा फेल होता है कि जाति के मसले को चिह्नित नहीं कर पाया जो भारत में बहुत बड़ा मसला था. हालांकि, उसका भी आधार शुरू में आर्थिक रहा है, लेकिन बाद में वह मानसिक स्तर पर चला गया. इसलिए इसकी लड़ाई भी साथ-साथ लड़नी बहुत जरूरी है. इसलिए इस संबंध में आंबेडकर और मार्क्स का एक साथ आना बहुत जरूरी हो जाता है. हाल में कैंपसों में बड़ा ध्रुवीकरण हुआ है.’
भाकपा माले की कार्यकर्ता कविता कृष्णन आंबेडकरवादी और मार्क्सवादियों के साथ आने को वक्त की जरूरत बताते हुए कहती हैं, ‘क्योंकि आज जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, वह खतरनाक है. आंबेडकरवादी और मार्क्सवादी ही नहीं, मुझे तो लगता है कि आंदोलनकारी जितनी ताकतें हैं, गांधीवादी भी, समाजवादी भी, आपस में बहसें करते हुए एकता को मजबूत कर सकते हैं. इसकी जरूरत सब महसूस कर रहे हैं. यह कोई बड़ी पार्टियों के स्तर से नहीं तय हुआ है. यह एकता स्वाभाविक रूप में आंदोलनों में बढ़ी है. क्योंकि जो हमला हो रहा है, वह काॅरपोरेट गाइडेड फासीवादी हमला है जिसमें वामपंथी और आंबेडकरवादी छात्रों को निशाना बनाया गया. दूसरी ओर कई दलित पार्टियां सत्ता में भागीदार भी हैं. तो जो युवा तबका है, उसे लगता है कि एक ऐसे राजनीतिक मॉडल की जरूरत है जो आंबेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए और वामपंथी आंदोलन के साथ भी मजबूती स्थापित करे.’
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी और आइसा के कार्यकर्ता रामायण राम कहते हैं, ‘यह भगत सिंह और आंबेडकर को एक साथ याद करने का समय है. क्योंकि उन्हीं के विचारों के आधार पर शोषणमुक्त समाज बन सकता है. आज जब राष्ट्रवाद की नई और संकीर्ण परिभाषा गढ़ी जा रही है तब आंबेडकर याद आते हैं. हमें उनकी संकल्पनाओं को स्वीकार करने की जरूरत है. आज वर्णव्यवस्था का समर्थन हो रहा है, भेदभावपूर्ण जातिवाद को संस्थाबद्ध करने की कोशिश की जा रही है. देश भर के विश्वविद्यालयों में जातीय युद्ध छेड़ा जा रहा है और ऐसा करने वाले भी आंबेडकर का नाम ले रहे हैं. जाति उन्मूलन ही बाबा साहब के राष्ट्रवाद का आधार था. बाबा साहब का कहना था कि दस सालों में लोकतांत्रिक ढंग से राजकीय समाजवाद लागू हो. हमें उनके इस सपने को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है.’
जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के शोध छात्र रमाशंकर सिंह का मानना है, ‘आज जब विश्वविद्यालयों में जय भीम, लाल सलाम का नारा लग रहा है तो इसे तात्कालिक रूप से ही नहीं देखना होगा. इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है. पिछले साल बांदा जिले में सम्मेलन हुआ जिसमें मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, अनीता भारती, आनंद तेलतुंबड़े ने हिस्सा लिया. इसमें प्रकाश करात भी आए थे. कहा गया कि किसान, मजदूर, दलित और स्त्री की मुक्ति के समान धरातल मार्क्स और आंबेडकर के बताए रास्ते से ही आ सकते हैं.’
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा अपना नाम न छापने की शर्त पर कहती हैं, ‘आज गहराते आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक संकट में आंबेडकरवादियों और मार्क्सवादियों का नजदीक आना जरूरी व स्वागत योग्य है. लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी हैं. आंबेडकरवाद सवर्ण वर्ग को ही अपना मूल शत्रु मानता है. निश्चित तौर पर, सवर्ण वर्चस्व व मानसिकता के खिलाफ संघर्ष जरूरी है, लेकिन क्या यह संघर्ष पूंजीवादी आर्थिक संकट, अभाव, शोषण व गैर-बराबरी, पूंजीवादी मुनाफे की लूट के खिलाफ भी होगा? मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र-नौजवान, महिला- इनके कॉमन प्रश्न क्या आंदोलन के केंद्र बनेंगे? सामाजिक आंदोलनों से कटे रहने और अपनी गंभीर ऐतिहासिक गलतियों के चलते समाज में अपना प्रभाव नहीं बना पा रहे प्रमुख मार्क्सवादी दल बढ़ते फासीवादी खतरे से निपटने के लिए यह शॉर्ट कट अपना रहे हैं, ताकि समाज के एक हिस्से में अपनी जगह बना सकें.’
हालांकि, रमाशंकर इन नए गठजोड़ को लेकर आशान्वित हैं. वे कहते हैं, ‘एक तरफ आंबेडकर हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों में इस विचार को आगे बढ़ाते हैं कि लोकतंत्र से ही वंचना और बहिष्करण से मुक्ति मिलेगी, बराबरी और अधिकार से ही दुनिया समान होगी. तो दूसरे छोर पर मार्क्स हैं जो पूंजी और समाज के रिश्ते को समझाकर उसे आम जनता के पक्ष में लाना चाहते हैं. मार्क्स और आंबेडकर के अनुयायी समाज को आमूलचूल बदलना तो चाहते रहे हैं लेकिन वे ऐसी किसी दृष्टि का विकास करने में असफल रहे जो एक वैकल्पिक राजनीतिक समाज बना सके जिसमें दलित, मजदूर, स्त्री, अल्पसंख्यक का शोषण न हो. अब एक ऐसा समय है कि जहां युवा, किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और अल्पसंख्यक नवपूंजीवादी ब्राह्मणवादी सत्ताओं से दबाए जा रहे हैं और यही समूह इतिहास को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है. जब रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं, सरकारें अपनी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाह रही हों और उन्हें फासीवादी पूंजीवाद का सहारा मिल रहा हो तो आंबेडकर और मार्क्स की गतिकी से एक मदद मिल सकती है.’
दूसरी ओर आंबेडकर को अपनाने लेने के लिए मचे सियासी हड़कंप पर भी सवाल उठ रहे हैं. पत्रकार अजय प्रकाश ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, ‘देश के आखिरी आदमी के नेता आंबेडकर की इतनी ऊंची बोली पहली बार लगी है. जिसे देखो वही आंबेडकर को अपनी ओर घसीट रहा है. समझ में नहीं आ रहा कि राजनीतिक पार्टियों का यह हृदय परिवर्तन उनको बाजार में नीलाम करने के लिए है या फिर मंशा कुछ और है. ऐसे में मैं इस आशंका से उबरने के लिए एक जानकारी चाहता हूं कि क्या आप 6 लाख गांवों के इस देश में ऐसे छह गांव भी जानते हैं जहां दलितों के साथ भेदभाव और छुआछूत नहीं होती? छह छोड़िए, एक ही बता दीजिए. अगर नहीं तो आंबेडकर को अपने-अपने पाले में घसीटना छोड़कर पहले एक ऐसा गांव बनाइए और भरोसा रखिए वहां आंबेडकर खुद चलकर आ जाएंगे. आपको खुद के आंबेडकरवादी होने की बांग नहीं देनी पड़ेगी.’
वामपंथ और आंबेडकरवाद के बीच कोई सियासी सामंजस्य हो सकता है या नहीं, भविष्य में राजनीतिक मोर्चा जैसी कोई संभावना हो सकती है या नहीं, इस सवाल पर पत्रकार और जेएनयू के शोध छात्र दिलीप मंडल कहते हैं, ‘दलित आंदोलन की तरफ से मार्क्सवाद की तरफ कोई हाथ बढ़ाया गया हो, इसके मुझे कोई संकेत नहीं दिखे हैं. मार्क्सवादी पार्टी के रहते हुए आंबेडकर ने अपनी पार्टी बनाई थी. उसकी जरूरत महसूस की थी. उनके लिए जाति का सवाल बहुत जरूरी था, सामाजिक लोकतांत्रिक समाज बने, यह सवाल बहुत जरूरी था. चूंकि लेफ्ट ने इस इश्यू को सीधे-सीधे कन्फ्रंट नहीं किया, इसलिए इस पार्टी की जरूरत महसूस की गई थी. आप कांशीराम को देखेंगे तो उन्होंने भी एक प्रयोग किया. वाम पार्टियों के रहते हुए भी आंबेडकरवादी आंदोलन का स्पेस था और लोगों ने अपने ढंग से काम करने की कोशिश की. नई चीज जो हुई है कि लेफ्ट ने पहली बार, अपने हाशिये पर चले जाने के दौर में, ये कोशिश की है कि जाति के सवाल को एड्रेस करें. पहली बार उन्होंने जातियों के सवाल पर सम्मेलन किए. पार्टी का ढांचा बदलने की बात की, हालांकि अभी तक हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि जो सवर्ण वर्चस्व था पार्टी में उसको तोड़ने की कोशिश की हो. कुल मिलाकर एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है. मुझे लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए कि चीजें कहां तक जाती हैं. अभी यह दोतरफा प्रक्रिया नहीं है. उधर से चार कदम आगे बढ़े तो इधर से एक कदम कोई बढ़ाए, ऐसा मुझे नहीं दिखता. कैंपसों में जरूर वाम और आंबेडकरवादियों के बीच एक सिंथेसिस बना है, लेकिन कैंपस में वाम पर दलित लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है.’

आजादी की लड़ाई के समय से ही आंबेडकर की अपनी अलग लड़ाई रही थी, क्योंकि वे जातीय शोषण और भारतीय समाज की विषमता को खत्म किए बगैर दलित समाज की मुक्ति को असंभव मान रहे थे. इसलिए मार्क्सवाद से भी उनकी दूरी बनी रही. मार्क्सवादी रुझान के दलित लेखकों को यह उम्मीद है कि अगर मार्क्सवादी अपने विचारों और संगठनों में कुछ संशोधनों के साथ दलितों को जगह दें तो दोनों मिलकर बेहतर राजनीतिक विकल्प बन सकते हैं. लेखक कंवल भारती कहते हैं, ‘मार्क्सवादियों ने आंबेडकर के जमाने में उनको नकार दिया था, लेकिन आज उनको स्वीकार करने के लिए विवश हो रहे हैं वोट की राजनीति की वजह से. आंबेडकर ने तो जब लेबर पार्टी बनाई थी, उस समय कहा था कि जितनी भी सोशलिस्ट ताकतें हैं, वे सब हमारे साथ आ जाएं और मिलकर एक जॉइंट फ्रंट बनाएं. लेकिन उस समय तक कोई भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था. आज से 20-25 साल पहले नंबूदरीपाद तक आंबेडकर को साम्राज्यवाद का पिट्ठू कह रहे थे. आज वही वामपंथी आंबेडकर के साथ आने को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने आंबेडकर को भारतीय संदर्भ में समझने की कोशिश की है. मैं तो शुरू से कहता हूं कि वामपंथी विचारधारा जब तक भारतीयकरण नहीं करेगी अपनी राजनीति का, तब तक वह इस देश में विकल्प नहीं बन सकती.’
राजनीतिक संभावनाओं के सवाल पर कंवल भारती कहते हैं, ‘बाबा साहब पूरे मार्क्सवादी थे, पूरे समाजवादी थे. वे चाहते थे कि सब समाजवादी ताकतें मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाएं. अगर ऐसा हुआ होता तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती ही नहीं. लेकिन ऐसी ताकतें कांग्रेस की पिछलग्गू थीं.’
वामपंथी बुद्धिजीवियों के बीच भी इस मसले पर बहस छिड़ चुकी है. मार्क्सवाद हर समस्या के मूल में वर्ग को देखता है तो आंबेडकरवाद जाति के सवाल के बिना आगे नहीं बढ़ता. हाल ही में बांदा में प्रकाश करात के बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक अरुण माहेश्वरी ने एक लेख में लिखा है, ‘मार्क्सवाद किसी भी संरचना के लक्षणों की, उसकी दरारों की पहचान कराता है. जाति से अगर वर्ग बनते हैं तो जातियों का अंत वर्ग का अंत नहीं हो सकता. यह एक संरचना का टूटना और उसकी जगह दूसरी संरचना का निर्माण है. इसीलिए कम्युनिस्टों ने जातिवाद के विरोध के साथ ही वर्ग संघर्ष पर हमेशा बिल्कुल सही बल दिया है. जातिवाद का खात्मा तो पूंजीवाद के विकास से भी होगा, लेकिन जातिवाद के अंत से पूंजीवाद का अंत नहीं होगा… आज जो लोग कम्युनिस्ट आंदोलन में आए गतिरोध के कारण जातिवाद के मसले के प्रति कम्युनिस्टों के नजरिये में किसी प्रकार के दोष में देख रहे हैं, वे पूरे विषय को सिर के बल खड़ा कर रहे हैं. कम्युनिस्ट आंदोलन को अपनी विफलता के कारण अपनी राजनीतिक कार्यनीति और सांगठनिक नीतियों की कमियों में खोजना चाहिए. मुश्किल यह है कि ऐसा करने पर पार्टियों के प्रभावी नेतृत्व की क्षमताओं पर सवाल उठने लगेंगे, जो कोई करना नहीं चाहता.’
[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
वामपंथियों ने कभी सामाजिक प्रश्न पर विचार नहीं किया : अभय कुमार दुबे
वामपंथी पार्टियों ने कभी सामाजिक प्रश्न पर पुनर्विचार नहीं किया. पार्टियों की जो लाइन तय की जाती है उसमें सामाजिक प्रश्न नहीं आए, जबकि आरएसएस इस पर व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है. वह वैदिक ज्ञान और आधुनिक संविधान में एक सूत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. वामपंथी सही सवाल क्यों नहीं उठा रहे? वे दलितों के सवाल से बचते क्यों हैं? दलितों के सवाल बड़े जटिल हैं, क्योंकि वे असुविधा पैदा करते हैं. कम्युनिस्ट पार्टियां दलित विमर्श और आंबेडकर के विचारों के जरिए अपना पुनर्संस्कार कर पाएं, इसके लिए तो उन्हें अपने विचारों में संशोधन करना चाहिए.
सीपीआई एमएल ने थोड़ा-सा वर्ग से अलग हटकर दलित महासभा बनाने का भी प्रयोग किया था. लेकिन उनका प्रयोग दो महीने नहीं चला. ऐसा क्यों हुआ? ये सीपीआईएमएल वही पार्टी है जिसको, जब मैं दिल्ली आया था तब दिल्ली के वामपंथी सर्किल में चमार पार्टी कहा जाता था. तो ऐसी पार्टी जिसे गरीबों और भूमिहीन दलितों का समर्थन हासिल था, उसने दलित महासभा बनाई तो वह दो महीने भी नहीं चली. इसकी सीधी वजह यह है कि जब तक आप सिर्फ वर्ग के सवाल पर फंसे रहेंगे तब तक न तो जाति के सवाल पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, न ही जेंडर के साथ गंभीरता से विचार कर पाएंगे.
जो हो रहा है वह तो ऐतिहासिक है. मैं पिछले तीस सालों से राजनीति में दिलचस्पी रखता हूं, जो हो रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा. लेकिन इसकी सीमा है कि ये छात्रों तक सीमित है. ये अभी कैंपस पॉलिटिक्स तक ही सीमित है. ज्यादा से ज्यादा बाहर जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग तक है, जो छात्रों के मुखातिब बहुत कम होता है. छात्रों में भी यह उन छात्रों तक सीमित है जिनमें से बहुत-से अब छात्र नहीं रहे. इस चीज का अगर हम लोग लाभ उठाना चाहते हैं और इस मुद्दे पर कोई ठोस और दीर्घकालिक राजनीति करना चाहते हैं, तो इस बारे में राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा. जब तक राजनीतिक दल इस विषय पर नहीं सोचेंगे, तब तक यह मसला केवल लेखक संघों और छात्रसंघों द्वारा ही संचालित किया जा सकता है. और राजनीतिक दल कब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ये मुझे नहीं पता. राजनीतिक दल अपनी सोच और अपनी स्थापित राजनीति बड़ी मुश्किल से बदलते हैं. उनको सामाजिक रूप से बहुत बड़ा धक्का लगता है तब वे अपनी रणनीति बदलते हैं. अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आई है कि वे इस दिशा में सोचें. इसका जो तुरंत राजनीतिक लाभ होगा, मुझे लगता है कि भाजपा रोहित वेमुला प्रकरण से पहले परमानेंट एलेक्टोरल बैलेट डेफिसिट के साथ आती थी और वो था अल्पसंख्यकों का घाटा. उसके पास अल्पसंख्यकों का घाटे का खाता था. अगर स्थिति इसी तरह से आगे बढ़ती रही और भाजपा अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर काटने की कोशिश करती रही तो उसका एक दूसरा परमानेंट डेफिसिट का खाता खुल जाएगा, वह है दलितों का खाता. अब देखने की बात है कि आगे क्या होगा.
(राजनीतिक विश्लेषक हैं. लेखक संगठनों के कार्यक्रम में दिए वक्तव्य के अंश)
[/symple_box]