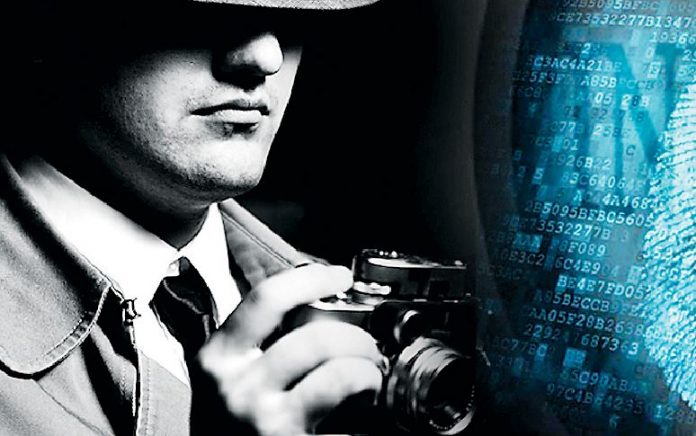आई.बी. सिंह
राजीव गाँधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए यह कहा था कि दिल्ली से जो एक रुपया देश के किसी गाँव के लिए भेजा जाता है, उसमे से कुल 15 पैसे ही वह गाँव तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि यह उन्हीं के शासन में होता था। यह पहले भी होता रहा है और आज भी होता है। शासक कितनी भी डींगें मार लें कि अब तो सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में रुपये पहुँच रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, परन्तु सत्यता यही है कि जो स्थिति राजीव गाँधी जी के समय में थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदहारण गाँव में चलने वाले मनरेगा के निष्पादन में व्याप्त भ्रष्टाचार है। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि बादशाह ने एक भ्रष्ट कर्मचारी को लहरें गिनने के काम में लगा दिया कि वहाँ वह भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, परन्तु उसने लहरें गिनने के नाम पर सभी नावें रोककर पैसे कमाने शुरू कर दिये। हम लोग उसको तारीफ़ की निगाह से देखने लगते हैं। प्रेमचंद के नमक का दारोग़ा के बंशीधर को आज के हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में 95 फ़ीसदी लोग नहीं जानते हैं। हम यह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हमारी नस-नस में समा गया है।
सन् 2014 के पूर्व जब पिछली सरकार थी, तब एक से बढक़र एक बड़े-बड़े घोटाले हुए, जैसे- 2जी घोटाला, कोयला खदान घोटाला, बैंक घोटाला, किंगफिशर के माल्या द्वारा किया गया घोटाला। इस सरकार के आने के बाद नीरव मोदी कांड, रोटो मेट घोटाला, यस बैंक घोटाला, पीएमसी बैंक घोटाला, यूपीपीसीएल प्रोविडेंट फंड काण्ड आदि घोटाले हुए, जिसमें एक साथ हज़ारों-लाखों करोड़ की लूट हो गयी और आम जनता बैठी देखती रह गयी। अभी हाल ही में राफेल मामले में भी मौज़ूदा केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगा है।
एक आँकड़े के अनुसार, जो बड़े-बड़े उद्योगों को लगाने के लिए और बड़े व्यापार करने के लिए, बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपये पूँजीपतियों को दिये जाते हैं और जो लौटकर नहीं आते, उन्हें सरकार एनपीए अकाउंट में डाल देती है। इस प्रकार से उच्च कोटि के भ्रष्टाचार के कारण सरकार को नुक़सान होता है और जो एनपीए अकाउंट में डाल दिया जाता है, वह राशि लगभग 21 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम रक़म है। परन्तु आम आदमी को उन बड़े घोटालों की फ़िक्र अधिक नहीं होती है। वह उस भ्रष्टाचार से सीधा प्रभावित होता रहता है, जिसमें उसे अपने थोड़ी-सी आमदनी में से निकालकर हज़ार-पाँच सौ रुपये पुलिस वाले को या शिक्षा विभाग, राशन विभाग, महापालिका के अधिकारी को, बिजली विभाग के कर्मचारी को, इंजीनियर, लेखपाल, पटवारी को या किसी प्रमाण-पत्र के लिए आदि अनेक विभाग हैं, जहाँ उसे आये दिन रिश्वत देनी पड़ती है।
आम आदमी ऐसे भ्रष्टाचार से सीधा प्रभावित होता है, जहाँ गाँव के सडक़, स्कूल, अस्पताल के नाम पर पैसा आता है और लुट जाता है। यहाँ हर क़दम पर, हर मोड़ पर लहरें गिनने वाले बैठे हैं और सरकारों ने उनकी ओर देखना ही बन्द कर दिया है, अर्थात् उन्हें लूटने की पूरी छूट दे दी गयी है। पूर्व में समय-समय पर पुलिस सुधार के लिए जो सुझाव दिये गये थे, वो आज की नयी तकनीकि, नये नियम, नयी व्यवस्था में महत्त्वहीन हो चुके हैं। ऐसे में कुछ ऐसा प्रभावशाली करने की ज़रूरत है, जो आम आदमी को शीघ्रता शीघ्र इस सदियों पुरानी बीमारी को कम कर सके। उसके लिए मेरे अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव हैं :-
क़ानून में हों क्या-क्या सुधार?
1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1947 में लागू किया गया था। उसे सन् 1964 में सनाथनम समिति के रिपोर्ट की संस्तुतियों के बाद यथोचित संसोधित किया गया। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1947 दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और दोनों के बीच के भ्रम को दूर करने के लिए 1988 में दूसरा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया। ‘यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन’ में लिये गये निर्णयों को लागू करने के लिए सन् 2018 में पुन: सन् 1988 के अधिनियम में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं।
2. यह कहा जा सकता है कि सन् 2018 के संशोधन के बाद आज जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू है, उसकी सभी परिभाषाएँ’, जैसे कि सरकारी कर्मचारी (पब्लिक सर्वेंट), अनुचित लाभ (अनड्यू एडवांटेज), सन्तुष्टि क़ानूनी पारिश्रमिक (ग्रैटीफिकेशन, लीगल रेम्युनेरेशन), सार्वजनिक कर्तव्य (पब्लिक ड्यूटी) आदि शामिल हैं; वह पूर्ण रूप से पर्याप्त हैं। अब उनमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. सन् 2018 के संशोधन की धारा-13 में आपराधिक कदाचार (क्रिमिनल मिसकंडक्ट) की परिभाषा, जो स्थानापत्र (सब्स्टीट्यूट) किया गया है, वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने में सहायक है। मेरे विचार से पूर्व में सन् 1988 के क़ानून में जो आपराधिक कदाचार की परिभाषा थी, वह बहुत व्यापक व प्रभावशाली थी और उसमें भ्रष्टाचार में पकड़े जाने वाले अपराधियों के बच निकलने की सम्भावना बहुत कम थी। यह कहा जा सकता है कि धारा-13 में जो संशोधन किया गया है, वह अभियुक्तों के हित में जा सकता है।
4. इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा-13 में जो सज़ा का प्रावधान है, उसे भी अपराध की श्रेणी के अनुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। जैसे धारा-13 में कम-से-कम 4 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। यह तो ठीक है; परन्तु जो अधिक से अधिक 10 वर्ष की सज़ा का जो प्रावधान है, उसे 14 वर्ष तक या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करने की आवश्यकता है।
5. सन् 2018 के संशोधन में धारा-17(ए) जोड़ी गयी है, उसमें उच्च पदों पर जो लोग नीति निर्णय (पॉलिसी डिसीजन) लेते हैं, उन्हें इतनी सुरक्षा दी गयी है कि उनके विरुद्ध कोई तहक़ीक़ात या जाँच शुरू होने के पहले, उनके नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। मेरे विचार से यह अनुपयुक्त है और इस प्रावधान को तुरन्त ही हटा देना चाहिए। जब तक जाँच नहीं होगी, तब तक यह पता ही नहीं चलेगा कि उक्त अधिकारी ने लोकहित में निर्णय लिया है या किसी भ्रष्टाचार के उद्देश्य से। जब न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के संस्तुति की आवश्यकता है ही, तब जाँच शुरू होने के पहले संस्तुति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दोहरे कवच के कारण उच्च पदों पर बैठे लोगों, जो नीति निर्णय लेते हैं; को भ्रष्टाचार करने की नीयत से निर्णय लेने की पूरी छूट मिल जाएगी। मेरी जानकारी में ऐसे कुछ मामले हैं।
6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यह प्रावधान है कि अपराध चाहे पाँच रुपये के लिए किया गया हो, या पाँच लाख करोड़ रुपये के लिए; एक ही सज़ा होगी। इस अधिनियम में अधिक-से-अधिक सज़ा सात वर्ष की जेल और ज़ुर्माना हो सकता है। मात्र धारा-13 में 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। मेरे विचार से इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।
7. इसको तीन श्रेणी में बाँटा जा सकता है। पाँच हज़ार तक की धनराशि तक के लिए किये गये अपराध को निम्न श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार से पाँच हज़ार या उससे ऊपर और पाँच लाख तक के धनराशि के लिए किये गये अपराध को मध्य श्रेणी के अपराध की संज्ञा में रखा जा सकता है। और पाँच लाख से ऊपर किसी भी धनराशी के लिए किये गये अपराध को उच्च श्रेणी के अपराध की संज्ञा में रखा जाना चाहिए।
8. उदहारण के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेज एक्ट-1985 में कुछ इसी तरह का प्रावधान था कि यदि अपराध पाँच मिलीग्राम तथ्य के लिए किया गया हो या पाँच कुंतल के लिए; सज़ा कम-से-कम 10 वर्ष का ही था। परन्तु 2 अक्टूबर, 2001 को अधिनियम में संशोधन करके उसमें अपराध को तीन भाग में बाँटा गया, जिसमें अपराध को स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी की परिभाषा में रखा गया और उसके अनुसार सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। संशोधन के पश्चात् स्मॉल क्वांटिटी के लिए छ: महीने तक की सज़ा, मीडियम क्वांटिटी के लिए 10 वर्ष तक की सज़ा और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए कम-से-कम 10 वर्ष के सज़ा का प्रावधान है। ऐसा ही प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी किया जा सकता है।
9. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सभी अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। किसी भी अपराध को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए।
10. वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट) व उससे जुड़े सभी सम्बन्धित अपराधों के लिए लाभार्थी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के प्रमुख पदों पर आसीन, जैसे कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जैसे लोगों के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए।
11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के परिक्षण और उसके निस्तारण में समय बचने के लिए यह प्रावधान भी रखा जा सकता है कि वो अभिलेख, जो विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्त के क़ब्ज़े से बरामद किया गया हो; उन अभिलेखों पर सम्बन्धित व्यक्ति के हस्ताक्षर को साक्ष्य रूप में इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाए कि उन्हें अभियुक्त को खण्डन (रिबटल) का अधिकार रहेगा।
एक ही केंद्रीय जाँच संस्था
1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित सभी अपराधों के जाँच के लिए केंद्रीय संस्थाओं में ले-देकर एक मात्र केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन यानी सीबीआई) ही एकमात्र प्रभावकारी जाँच संस्था (इन्वेस्टीगेशन एजेंसी) है। उसको भी कभी अदालतों के आदेश से और कभी राज्य सरकारों के माँग पर, भ्रष्टाचार सम्बन्धित अपराधों के अतिरिक्त का भी काम दे दिया जाता है, जिसमें उनका काम मुख्य उद्देश्य से भटककर अन्यत्र चला जाता है।
2. इसके अतिरिक्त सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थानपना अधिनियम-1965 (डेल्ही पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट-1965) के प्रावधान के तहत किया गया है, जो स्वयं में आज तक विवादित है कि यह एक वैधानिक संस्था है या नहीं। यह विवाद अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में मेरे विचार से एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, संसद के द्वारा पारित अधिनियम से स्थापित किया
जाना चाहिए।
3. ऐसे भ्रष्टाचार निवारण संगठन के स्वतंत्र शाखाएँ होनी चाहिए, जो विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने, उन विभागों में होने वाले अपराधों की जाँच करने, अपराध सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्रित करने और अपरधियों को न्यायालय में उनके द्वारा किये गये अपराधों की सज़ा दिलवाने का काम करे। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, रेलवे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जीएसटी, पेट्रोलियम आदि-आदि। ऐसे सभी महत्त्वपूर्ण विभागों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र संवर्ग (इनडिपेंडेंट काडर) की एक सतर्कता / जाँच / सूचना विभाग होना चाहिए, जो अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी क़दम उठाए।
4. इन सभी विभागों के जाँच एजेंसी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र संवर्ग के रूप में रखा जाए। परन्तु जैसा कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेज एक्ट-1985 में यह प्रावधान है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जाँचकर्ता या अपराध को रोकने वाले अधिकारी के कार्य में सहयोग करें। ऐसा ही प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत भी होना चाहिए, जिससे दूसरे किसी भी विभाग का अधिकारी, अपराधी या अपराध को सीधे या परोक्ष रूप से प्रश्रय न प्राप्त हो सके, उसको रोके और अपराधी को बचने का भी अवसर न प्राप्त हो सके।
5. स्वतंत्र संवर्ग का एक विशेष कारण यह भी है कि आज के युग में जब हर दिन नयी-नयी तकनीकि निकल रही है, अपराधी भी उतनी ही तेज़ी से उसमें कमियाँ ढूँढकर भ्रष्टाचार का रास्ता ढूँढ लेते हैं। यदि जाँच अधिकारी का एक ही काडर होगा, तो वह अपने विभाग और क्षेत्र में अपराधी के बराबर की तकनीकि और उसकी सोच व तरीक़े का मुक़ाबला करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए बिजली विभाग के एक जाँच अधिकारी को उस विभाग के तकनीकि सीखने में ही वर्षों लग जाते हैं, तब तक अपराधी चोरी और बेईमानी करता रहता है और जब तक यह सब जाँच अधिकारी को समझ में आता है, तब तक उसका तबादला किसी दूसरे विभाग में कर दिया जाता है।
6. इसके अतिरिक्त प्रभावशाली ढंग से जाँच के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी भी अपराध के लिए यथासम्भव एक ही जाँच अधिकारी या एक जाँच अधिकारी के नेतृत्व में एक ही टोली (टीम), अपराध की जाँच करे। इसका एक यह भी लाभ होगा कि सत्र परिक्षण के अन्त में त्रुटिपूर्ण या बेईमानी के जाँच के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।
7. अपराध की सूचना देने वाले की पहचान को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाए। सही सूचना देने वाले को अपराधी की सज़ा होने पर ईनाम का प्रावधान होना चाहिए। इसी प्रकार से जानबूझकर या द्वेष की भावना से ग़लत सूचना देने वाले का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसे भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इससे ईमानदार व्यक्ति के विरुद्ध द्वेषपूर्ण शिकायतों में कमी आएगी।
राज्य सरकारों की जाँच संस्थाएँ
1. राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले पुलिस विभाग की तो और भी हालत दयनीय है। एक दारोग़ा जो आज चौराहे पर यातायात नियंत्रण कर रहा होता है, उसे दूसरे ही दिन किसी नेता के सुरक्षा में लगा दिया जाता है। फिर किसी जाँच में लगा दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में समाज और सरकार के विभाग बँटे हुए हैं? इसकी गिनती भी करना मुश्किल है। जैसे संगीत, शिक्षा के कई स्तर, विश्वविद्यालय की डिग्री सम्बन्धित अपराध, बिजली विभाग, चिकित्सा, शिक्षा चिकित्सा, महापालिका आदि। ऐसे में एक साधारण से पुलिस वाले से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह सभी क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त कर लेगा।
2. इसी कारणवश पुलिस जाँच में इतनी $खामियाँ रह जाती हैं कि मुक़दमे छूटने का फ़ीसद इतना रहता है कि कभी किसी के साथ न्याय हो पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार असल अपराधी के विरुद्ध आरोप पत्र ही नहीं प्रस्तुत हो पाता है और कभी-कभी पूर्ण निर्दोष के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाता है। यही नहीं, कई बार तो असल अपराधी साफ़-साफ़ बच जाता है और निर्दोष को सज़ा हो जाती है।
3. ऐसे में आवश्यकता है कि केंद्रीय विभागों और केंद्र सरकार से सम्बन्धित विभागों के जाँच के लिए जाँच संस्था का स्वतंत्र संवर्ग बनाकर केंद्र सरकार की ही तरह उन जाँच संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दिया
जाना चाहिए।
4. इसका एक लाभ यह भी होगा कि त्रुटिपूर्ण जाँच या बेईमानी से हुई जाँच में उत्तरदायित्व निर्धारित करने में भी आसानी होगी।
विशेष लोक-अभियोजक
1. जिस प्रकार से निष्पक्ष और योग्य जाँच अपराध के लिए उत्तरदायित्व ठहराने के लिए अभियुक्त निर्धारित करना आवश्यक होता है, उसी तरह उस अभियुक्त को न्यायालय से सज़ा दिलाने के लिए एक योग्य लोक-अभियोजक की भी आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुक़दमों को न्यायालय में प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और बहस के लिए एक स्वतन्त्र, योग्य और ईमानदार लोक-अभियोजक की भी आवश्यकता होती है।
2. अत: विशेष न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र विशेष लोक-अभियोजक का संवर्ग हो। इन लोक अभियोजकों को कम-से-कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए और इनकी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक सरकार के बनने पर सत्ताधारी पार्टी के चहेतों को लोक-अभियोजक बना दिया जाए और शासन परिवर्तन होते ही उन्हें हटा दिया जाए।
3. उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मुक़दमों की पैरवी के लिए इसी संवर्ग के विशेष लोक-अभियोजक के अधिकारियों को ही बहस और पैरवी के लिए पदोन्नति देकर ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। इससे संवर्ग के विशेष लोक-अभियोजकों के मन में और भी मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने की रुचि बढ़ेगी।
विशेष न्यायालय
1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यह प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों के परिक्षण के लिए विशेष अदालतें होंगी, जो किसी भी अपराध का सीधा संज्ञान लेंगी। उन मुक़दमों को दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के यहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
2. इसी प्रकार से वर्तमान अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यथासम्भव प्रतिदिन के हिसाब से किसी भी परीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी और दो वर्ष के अन्दर यथासम्भव परिक्षण सम्पन्न कर दिया जाएगा। और यदि दो वर्ष में कार्यवाही समाप्त नहीं हो पाती है, तो एक समय में कारण बताते हुए छ: माह तक के लिए कार्यवाही सम्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे विभिन्न कारणों से कभी भी क़ानून का पालन नहीं हो पाता है। इसे स$ख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है।
3. आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालतें लखनऊ और गा•िायाबाद में ही हैं। इतनी दूर और इतने कम विशेष न्यायालय होने के कारण मुक़दमों की सुनवायी में बहुत कठिनायी होती है। मेरे विचार से ऊपर लिखे गयी जाँच एजेंसीज के गठन के बाद एकाएक मुक़दमों की भरमार होगी। यह अत्यंत आवश्यक होगा कि विशेष न्यायाधीशों की अदालतें प्रत्येक ज़िले में उसी तरह बनायी जाएँ जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीडऩ अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की अदालतों की स्थापना प्रत्येक ज़िले में की गयी है।
4. अधिनियम में यह भी प्रावधान किया जाए कि सत्र परिक्षण के समापन के समय यदि मुक़दमा छूटता है, तो न्यायालय जाँच अधिकारी द्वारा जानबूझकर की गयी लापरवाही या किसी को लाभ पहुँचाने के लिए किये गये कृत्य के लिए उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित करे।
निचोड़
1. भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है, जो मानव उत्पत्ति के समय से ही तक़रीबन सभी देशों में क्षेत्र, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर हर स्थान और संस्था में व्याप्त है। हाँ, कभी और कहीं-कहीं यह कम होता है और कहीं बहुत अधिक भी होता है। परन्तु इसको रोकने का प्रयत्न सदैव से होता रहा है। इसे रोकना शासक की इच्छाशक्ति, ईमानदारी और प्रयत्न पर निर्भर करता है। इससे हारकर हाथ-पर-हाथ रखकर बैठ जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है।
2. यदि शासक और शासन एक बार ठान ले और इसे दूर करने की सोच लें, तो मानव कल्याण के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए भारत में उसी तरह से क़ानून, व्यवस्था और सज़ा का प्रावधान करना चाहिए जैसा कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेज के अपराधियों और बाल यौन शोषण करने वाले अपराधियों के साथ किया जा रहा है।
3. ऑस्टिन का सिद्धांत है कि प्रतिबन्ध या भय या कठोरता ही ऐसा उपाय है, जिससे अपराध को कम किया जा सकता है। भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए किसी भी उदारता का परिचय नहीं देना चाहिए। सरकार प्रत्येक वर्ष आम जनता के कल्याण के लिए एक-से-एक कर कई योजनाएँ बनाती है और उन्हें लागू करने के लिए कार्यपालिका पर छोड़ देती है। यदि भ्रष्टाचार से कठोरता से योजनाबद्ध तरीक़े से नहीं निपटा जाएगा, तो सरकार के जन-कल्याण के सारे प्रयत्न विफल होते रहेंगे।
4. मैं जो कुछ भी सुझाव दे सकता हूँ, वो सभी मेरे अपने अनुभवों पर आधारित हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरे सुझाव सर्वोत्तम हैं। परन्तु यदि सरकार की इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार को कम करने की है, तो इन पर जन-हित और देश-हित में विचार किया जा सकता है।
मुझे आशा है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जो जीरो टॉलरेंस (शून्य सहनशीलता) की बात कहती है; उसे लागू भी करेगी।
(लेखक लखनऊ उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी हैं।)